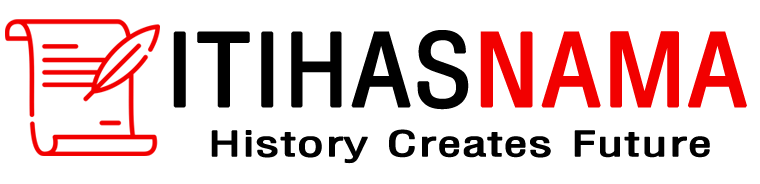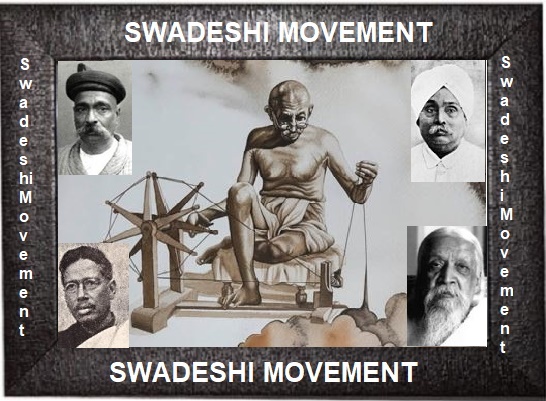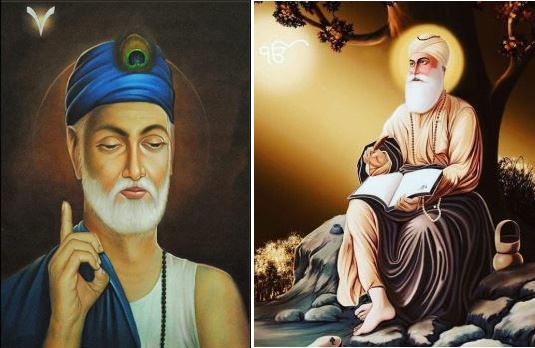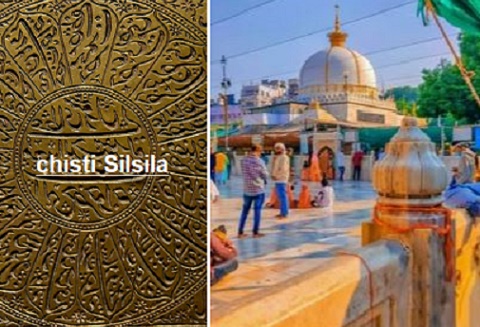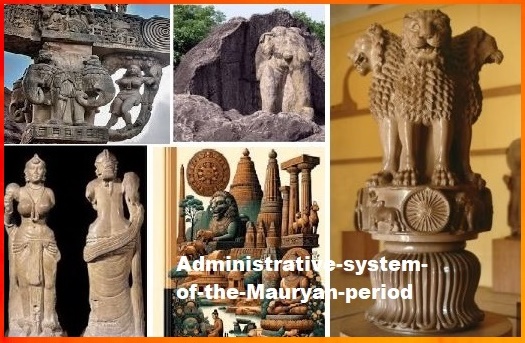
आचार्य चाणक्य (विष्णुगुप्त या कौटिल्य) के ‘अर्थशास्त्र’ एवं मेगस्थनीज की ‘इंडिका’, अशोक के शिलालेख तथा अन्य यूनानी कृतियों से मौर्यकालीन शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। मौर्य सम्राटों ने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की थी। सम्राट अशोक ने इस केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को ‘पितृवत निरंकुश राजतंत्र’ में परिवर्तित कर दिया। प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था।
आचार्य चाणक्य के सप्तांग सिद्धान्त के अनुसार, राज्य के निम्न सात अंग होते हैं- 1. सम्राट 2. अमात्य 3. जनपद 4. दुर्ग 5. राजकोष 6. सेना तथा 7. मित्र। राजा उपरोक्त सात तत्वों की आत्मा है। राजा सभी प्रकार की सत्ता का स्रोत एवं उसका केन्द्र बिन्दु, प्रशासन, विधि एवं न्याय का प्रमुख स्रोत तथा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, किन्तु वह निरकुंश नहीं होता था।
आचार्य चाणक्य कृत ‘अर्थशास्त्र’ के अनुसार, “प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है।” मौर्य राजाओं ने इन बातों को मानते हुए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। सम्राट अशोक ने अपने पांचवें शिलालेख में कहा है कि ‘सभी मनुष्य मेरी संतान हैं।’
केन्द्रीय प्रशासन
मौर्यकालीन केन्द्रीय शासन प्रणाली के तीन भाग थे — 1. राजा 2. मंत्रिपरिषद 3. विभागीय व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय प्रशासन में सम्राट अपने शासन कार्यों में मंत्रिपरिषद (अमात्यों, मंत्रियों तथा सैन्य अधिकारियों) की सहायता प्राप्त करता था। राज्य के सभी पदाधिकारियों को ‘अमात्य’ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार, सम्राट के बाद अमात्य का स्थान था। प्रथम श्रेणी के अमात्य को ‘मंत्रिन’ कहा जाता था, इन्हें 48000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। द्वितीय श्रेणी के अमात्य ‘मंत्रिपरिषद के सदस्य’ होते थे, इन्हें 12000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। जबकि तृतीय श्रेणी के अमात्य विभिन्न ‘विभागों के अध्यक्ष’ होते थे, इन्हें 1000 पण वार्षिक वेतन मिलता था।
मौर्य प्रशासन पूर्णत: केन्द्रीकृत नौकरशाही प्रशासन तंत्र था। कौटिल्य ने “राजा को 'धर्मप्रवर्तक' अथवा सामाजिक व्यवस्था का प्रवर्तक बताया था।” राजा को प्रशासन में मदद देने के लिए 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था जिसे ‘तीर्थ’ कहा जाता था, ये ‘महामात्य’ भी कहे जाते थे। तीर्थों में मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। मंत्रियों की नियुक्ति हेतु इनके चरित्र को जांचा-परखा जाता था, जिसे ‘उपधा परीक्षण’ कहते थे।
केन्द्रीय प्रशासन एक सचिवालय द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक अध्यक्ष अथवा अधीक्षक होता था। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी अध्यक्ष होते थे। अध्यक्षों को अमात्य वर्ग में भी नियुक्त किया जा सकता था। आचार्य चाणक्य ने 32 विभाग एवं उनके अध्यक्षों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं —
1. आकाराध्यक्ष - खान एवं धातुकर्म का प्रमुख अधिकारी 2. अक्षपटलाध्यक्ष -लेखा नियंत्रक। 3. आयुधागाराध्यक्ष - आयुध विभाग का अध्यक्ष 4. गणिकाध्यक्ष - मनोरंजन तथा वेश्यालयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। 5. कुप्याध्यक्ष - वन उत्पादों का प्रमुख। 6. लक्षणाध्यक्ष - टकसाल का प्रमुख 7. लवणाध्यक्ष - नमक का अधीक्षक 8. मद्राध्यक्ष - परिपत्र अधिकारी। 9. नागावनाध्यक्ष - हाथी वनपाल। 10. नावाध्यक्ष -जहाज वाहन नियंत्रक 11. कोषाध्यक्ष - राजकोष प्रमुख 12. ध्युताध्यक्ष - द्युतक्रीड़ा का अध्यक्ष। 13. बंधनागाराध्यक्ष - कारागार का अध्यक्ष(प्रशस्त्रि नामक अधिकारी भी जेलों की देखभाल करता था।) 14. अश्वाध्यक्ष - अश्वारोही सेना का प्रमुख 15. देवताध्यक्ष - मंदिरों का अध्यक्ष।
16. गो-अध्यक्ष -राजसी मवेशियों का अध्यक्ष 17. मनाध्यक्ष - सर्वेक्षक एवं समयपालक 18. पण्याध्यक्ष - राज्य व्यापार नियंत्रक 19. पौतवाध्यक्ष – माप-तौल का नियंत्रक 20. पत्याध्यक्ष - पैदल सेनाध्यक्ष 21. पत्तनाध्यक्ष - राज्य बंदरगाह का नियंत्रक 22. संस्थाध्यक्ष - निजी व्यापार नियंत्रक 23. सीताध्यक्ष - राजसी भूमि का अध्यक्ष 24. सूनाध्यक्ष - पशुओं का रक्षक एवं बुचड़खाना नियंत्रक 25. सुराध्यक्ष - मदिरा नियंत्रक 26. सुत्राध्यक्ष - वस्त्र आयुक्त 27. विविताध्यक्ष - चारागाह नियंत्रक 28. सुवर्धाध्यक्ष - कीमती धातु एवं आभूषण अध्यक्ष 29. शुल्काध्यक्ष - सीमा शुल्क एवं चुंगी नियंत्रक 30. कोष्टागाराध्यक्ष - गोदाम का अध्यक्ष 31. लोहाध्यक्ष - धातुओं का अध्यक्ष 32. रक्षाध्यक्ष - रथ सेनाध्यक्ष।
प्रान्तीय व्यवस्था
मौर्य साम्राज्य प्रान्तों में विभाजित था, चन्द्रगुप्त मौर्य ने शासन-सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को चार प्रान्तों में विभाजित किया था, इन प्रान्तों को ‘चक्र’ अथवा ‘आहार’ कहा जाता था। इन प्रान्तों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। किन्तु सम्राट अशोक के समय कलिंग विजय के पश्चात प्रान्तों की संख्या बढ़कर पांच हो गई। मौर्य साम्राज्य के पांच प्रान्त इस प्रकार थे —
1. उत्तरी प्रान्त (उत्तरापथ) की राजधानी तक्षशिला। इसमें पंजाब, कश्मीर, गान्धार तथा सिन्ध आदि प्रदेश शामिल थे।
2. पश्चिमी प्रान्त (अवन्तिपथ) की राजधानी उज्जयिनी। अवन्तिपथ में सौराष्ट्र, मालवा तथा राजपूताना के क्षेत्र शामिल थे।
3. पूर्वी प्रान्त (प्राच्यपथ) की राजधानी कलिंग (तोशाली) ।
4. दक्षिणी प्रान्त (दक्षिणापथ) की राजधानी सुवर्णगिरि। विन्ध्याचल के दक्षिण का समस्त प्रदेश।
5. केन्द्रीय प्रान्त अथवा गृह राज्य (मगध) की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सम्पूर्ण मौर्य साम्राज्य की केन्द्रीय राजधानी थी। केन्द्रीय प्रान्त में सम्राट स्वयं ही शासन करता था।
तक्षशिला तथा उज्जयिनी जैसे महत्वपूर्ण प्रान्तों का नियंत्रण सीधे ‘कुमारों’ अथवा ‘आर्यपुत्र’ नामक पदाधिकारियों के अधीन होता था। सम्राट बनने से पूर्व अशोक स्वयं उत्तरापथ एवं अवन्ति (उज्जयिनी) का ‘कुमार’ रह चुका था। रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, सौराष्ट्र (काठियावाड़) का गवर्नर पुश्यगुप्त वैश्व था। उसने सिंचाई के लिए ‘सुदर्शन झील’ का निर्माण करवाया था। अशोक के समय यहां का प्रान्तपति यवन जातीय तुषास्प था जिसने सुदर्शन झील से पानी के निकासी के लिए नहरें बनवाई थीं। दिव्यावदान के अनुसार, कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था।
कुमारामात्य की सहायता हेतु प्रत्येक प्रान्त में ‘महामात्र’ नामक अधिकारी होते थे। इनके अन्तर्गत विभिन्न विषयक पदों पर ‘सामन्त’ अथवा ‘विषयपति’ होते थे। मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत कुछ अर्द्धस्वशासित प्रदेश भी थे। यहां स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी किन्तु अन्तपालों द्वारा उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रहता था।
जिला प्रशासन
प्रत्येक प्रान्त मण्डलों में विभक्त थे। मण्डलों का शीर्ष पदाधिकारी ‘महामात्य’ होता था। तत्पश्चात प्रत्येक मण्डल विभिन्न जनपदों में विभक्त था। जनपद को जिला या स्थानीय कहते थे। जनपद का प्रशासक स्थानिक होता था। एक स्थानीय में तकरीबन 800 ग्राम होते थे। द्रोणमुख में 400 गांव, खार्वटिक में 200 गांव तथा संग्रहण में 100 गांवों का समूह होता था। प्रत्येक जनपद में तीन प्रमुख अधिकारियों का समूह होता था — प्रदेष्टि, राजुक तथा युक्त। प्रदेष्टि का कार्य निरीक्षण करना, राज्जुक का कार्य भू सर्वेक्षण एवं राजस्व निर्धारण तथा युक्त का कार्य लेखा व्यवस्था देखना था।
- प्रदेष्टि, राज्जुक तथा युक्त
प्रदेष्टि नामक अधिकारी समाहर्ता के अधीन कार्य करता था जो स्थानिक व गोप के कार्यों की जांच करता था। प्रदेष्टि प्रत्येक पांचवें वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रशासन का निरीक्षण करने के लिए दौरा करता था। जबकि राज्जुक भूमि के सर्वेक्षण एवं भूराजस्व निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता था। वहीं युक्त नामक अधिकारी सचिवालय कार्य तथा लेखा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य देखता था।
- गोप और स्थानिक
ग्राम स्तर तथा जनपद स्तर के बीच प्रशासन का एक माध्यमिक स्तर भी था। पांच अथवा दस गांवों की ईकाई होती थी, जिसका अधिकारी गोप तथा स्थानिक होते थे। गोप लेखाकार का काम करता था जबकि स्थानिक द्वारा ‘कर’ वसूली की जाती थी। गोप जनगणना पदाधिकारी भी होता था।
प्रशासन की सबसे छोटी ग्राम थी, ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था। अपराधों पर नियंत्रण हेतु पुलिस व्यवस्था थी, पुलिस को रक्षिण कहा जाता था।
नगर प्रशासन
अशोक के अभिलेखों में नगर प्रशासन से जुड़े उच्चाधिकारी को ‘महामात्र’ कहा गया है। मौर्य युग में नगर का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख ‘नागरिक’ अथवा ‘पुरमुख्य’ कहा जाता था।
हांलाकि आचार्य चाणक्य (कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त) ने नगर प्रशासन का वर्णन नहीं किया है, किन्तु मेगस्थनीज की कृति ‘इंडिका’ के अनुसार, “पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मण्डल द्वारा नियुक्त 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे।”
प्रथम समिति — उद्योग शिल्प का निरीक्षण। द्वितीय समिति — विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति — जन्म-मरण का रजिस्ट्रेशन। चतुर्थ समिति — व्यापार व वाणिज्य। पंचम समिति— निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ट समिति — विक्री कर वसूल करना। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज नगर आयुक्त को ‘ऐस्टोनोमोई’ कहता है, जबकि नगर में सड़क तथा भवन निर्माण अधिकारी को ‘एग्रोनोमोई’ कहा है।
अन्य इतिहासकारों से इतर रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य को तीन भागों में विभक्त बताया है।
1. महानगरीय राज्य — यह क्षेत्र सर्वाधिक केन्द्रीकृत था। इसके तहत मगध के आसपास का क्षेत्र आता था। इस क्षेत्र में सम्राट, सेनापति, मंत्री और सेना आदि रहती थी।
2. कोर राज्य — इस राज्य के तहत तक्षशिला, कलिंग आदि के राज्य आते थे, जिन पर सेना और पदाधिकारियों के द्वारा नियंत्रण की हर सम्भव कोशिश की जाती थी।
3. सीमापवर्ती राज्य — यह क्षेत्र आवटिक जनजातियों का था, यहां नियंत्रण सबसे कमजोर था।
मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था

मौर्य युग में सम्पूर्ण प्रशासन तथा अधिकारियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था, जिन्हें महामात्यसर्प कहा जाता था।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष (जासूस) कहा गया है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों के द्वारा देशी-विदेशी लोगों की गतिविधियों की पूरी जानकारी रखी जाती थी जो कि सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। गुप्तचर दिन-प्रतिदिन के कार्यों की सूचना सम्राट को दिया करते थे।
यूनानी इतिहासकार एरियन ने गुप्तचरों को ‘ओवरसियर’ तथा स्ट्रेबो ने ‘इंस्पेक्टर’ कहा है। ओवरसियर अथवा इन्सपेक्टर का कार्य नगर एवं जनपद के कार्यों का निरीक्षण करना था। नर गुप्तचरों को सन्ती, तिष्णा तथा सरद कहा जाता था जबकि महिला गुप्तचरों को वृषली, भिक्षुकी तथा परिव्राजक कहा जाता था।
अर्थशास्त्र के अनुसार, दो प्रकार के गुप्तचर होते थे— 1. संस्था - वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहकर संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते तथा राजकर्मचारियों (अमात्य, मंत्री आदि) के भ्रष्टाचार का पता लगाते थे। 2. संचार- ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते तथा राजा तक सूचना पहुंचाते थे।
संस्था गुप्चर पांच प्रकार के होते थे –
- कापाटिक - दूसरे के रहस्यों को जानने वाला विद्यार्थी भेष में रहने वाला गुप्तचर।
- उदास्थित - संन्यासी वेषधारी गुप्तचर।
- गृहपतिक - गरीब किसान वेश में रहने वाला गुप्तचर।
- वैदेहक - गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर।
- तापस - सिर मुंडाए अथवा जटा धारण किए तपस्वी वेश में गुप्तचर।
संचारा (भ्रमणशील) गुप्तचरों के प्रकार –
- सत्री - समुद्री विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, इन्द्रजाल, वशीकरण तथा नृत्य-संगीत में निपुण गुप्तचर।
- तीक्ष्ण - धन के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करने वाला गुप्तचर।
- सरद - अपने ही बन्धुओं से स्नेह नहीं रखने वाला, क्रूर तथा प्रकृति से आलसी गुप्तचर।
- परिव्राजका - संन्यासिनी वेष में गुप्तचर का कार्य करने वाली महिला।
गुप्तचर विभाग में संन्यासी, विद्यार्थी, गृहस्थ एवं विषकन्याओं की नियुक्ति की जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार, वेश्याओं को भी गुप्तचरों के पदों पर नियुक्त किया जाता था। यदि कोई गुप्तचर गलत सूचना देता था तो उसे दंडित किया जाता था अथवा उसे पद से मुक्त कर दिया जाता था। इस विभाग में वे ही नियुक्त होते थे, जो उपधा परीक्षण में उत्तीर्ण होते थे।
गुप्तचरों के अतिरिक्त शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस होती थी जिन्हें रक्षिन कहा जाता था। विदेशों में नियुक्त राजदूत खुले गुप्तचर होते थे। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिकाएं होती थी। मेगस्थनीज व स्ट्रेबो महिला अंगरक्षकों का उल्लेख करते हैं। महिला अंगरक्षकों को समारानुरांगिनी कहा जाता था।
गुप्तचरों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था — कूटनीतिक लेख का ज्ञान, गुप्त लिपि का ज्ञान, भेष एवं रूप बदलने में माहिर, विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता, अभिभाषण की कला, जनता की राय बदलने में माहिर, खान-पान, रहन-सहन, धन प्रयोग, विपत्तियों से बचाने का तरीका, औषधि प्रयोग, दुष्प्रचार अथवा अफवाह फैलाने की कला आदि।
सैन्य व्यवस्था
सेना के संगठन हेतु अलग से सैन्य विभाग था, जो छह समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इन समितियों के कुल 30 सदस्य सेना के पांच विभागों की देखरेख करते थे, जैसे — पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। सभी युद्ध आयुध एवं हथियार राज्य की ओर से प्रदान किए जाते थे। मौर्य सैनिक सामान्यतया तलवार, भाले, धनुष-बाण, कटार आदि शस्त्रों का अधिकाधिक प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त मौर्य सेना में ‘सर्वतोभद्र’ नामक एक ऐसा यंत्र होता था,जिससे शत्रु सेना पर पत्थरों की वर्षा की जाती थी। घायल सैनिकों के इलाज के लिए सेना के साथ वैद्य सर्वदा मौजूद रहते थे।
सैनिक प्रबन्ध देखरेख करने वाला अधिकारी अन्तपाल कहलाता था। यह सीमान्त क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। अन्तपाल नामक अधिकारी दुर्गों के भी अध्यक्ष होते थे। युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी सेनापति होता था। सेनापति मंत्रिण का सदस्य होता था। सेनापति को 48000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। सेना के चार अंगों- अश्व, गज, रथ, पैदल के अलग-अलग अध्यक्ष होते थे, जो सेनापति के अधीन कार्य करते थे। इन्हें 8000 पण वार्षिक वेतन मिलता था।
युद्ध क्षेत्र में नायक ही सेना का नेतृत्व करता था। नायक को 12000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में ‘नवाध्यक्ष’ के उल्लेख से यह जानकारी मिलती है कि मौर्यों के पास भी नौसेना थी। सर्वप्रथम ग्रुनवेडेल ने बताया कि मौर्यों का वंश चिह्न ‘मोर’ था।
इतिहासकार प्लिनी की ‘नेचुरल हिस्ट्री’ के अनुसार, “चन्द्रगुप्त मौर्य के पास छह लाख पैदल सैनिक, पचास हजार अश्वारोही, नौ हजार हाथी तथा आठ सौ रथों से सुसज्जित विराट सेना थी।” वहीं, जस्टिन ने “चन्द्रगुप्त की सेना को डाकूओं का गिरोह” कहा है। इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि “मौर्य सेना को सर्वशक्तिशाली बनाने का श्रेय चन्द्रगुप्त तथा उसके योग्य मंत्री चाणक्य को जाता है।” स्मिथ ने मौर्य सेना को अकबर की सेना से शक्तिशाली बताया है।
इसे भी पढ़ें : चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिन्दुसार का इतिहास