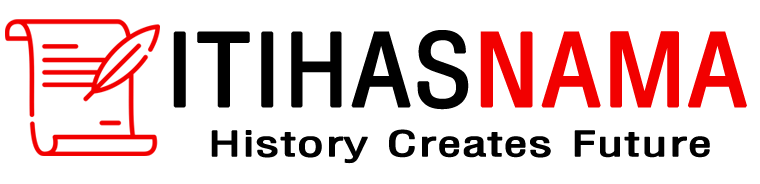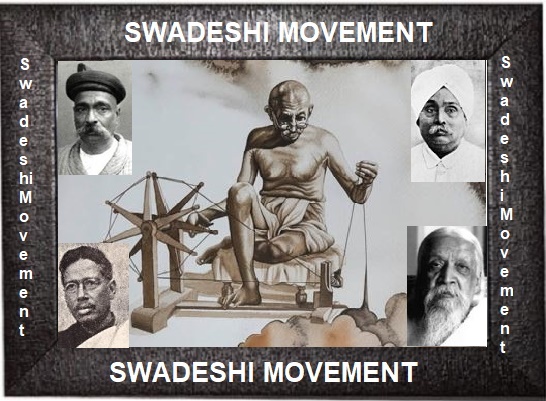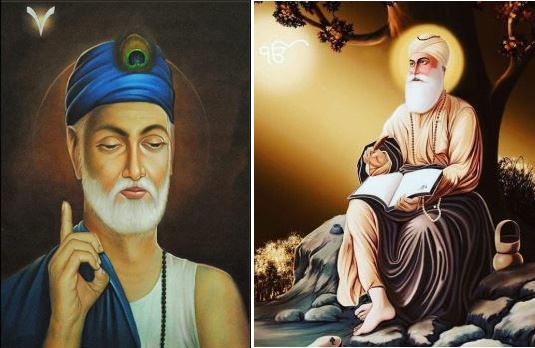भागवत धर्म के प्रवर्तक ‘वृष्णिवंशी’ या ‘सात्वतवंशी’ श्रीकृष्ण थे। श्रीकृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत (पूज्य) कहते थे। इसलिए इस धर्म का नाम ‘भागवत धर्म’ पड़ गया। भागवत धर्म का अन्य नाम सात्वत धर्म व पांचरात्र धर्म भी है। भागवत धर्म को ‘सात्वत धर्म’ इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण का सम्बन्ध ‘सात्वत वंश’ से जोड़ा जाता है।
ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकाण्ड तथा यज्ञीय व्यवस्था के विरूद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जन्में पहले सम्प्रदाय का नाम भागवत सम्प्रदाय है। भगवान कृष्ण के उपासक अथवा भक्त भागवत कहलाते थे। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनी के ‘अष्टाध्यायी’ से प्राप्त होता है।
भागवत धर्म का विकास
वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनी के ‘अष्टाध्यायी’ में ई.पू. पांचवी शती में मिलता है। वासुदेव की पूजा करने वाले ‘वासुदेवक’ कहलाते थे। पाणिनी के काल में भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले गृहपति को ‘भागवतम’ तथा गृहपत्नी को ‘भागवती’ कहा जाता था।
— भागवत धर्म के विषय में प्रारम्भिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव श्रीकृष्ण थे जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे।
— श्रीकृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छान्दोग्य उपनिषद में मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद में श्रीकृष्ण को देवकी का पुत्र व ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है।
— वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण ‘नारायण’ से किया गया। नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए।
— भागवत धर्म का सिद्धान्त ‘भगवद्गीता’ में निहित है। वासुदेव कृष्ण से जुड़ा भागवत सम्प्रदाय ‘सांख्य योग’ से सम्बन्धित था। इसमें वेदान्त, सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है।
— जैन धर्म के ग्रन्थ ‘उत्तराध्ययन’ में वासुदेव को ‘केशव’ नाम से पुकारा गया है, इस जैन ग्रन्थ में वासुदेव को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का समकालीन बताया गया है।
— भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। मेगस्थनीज ने ‘इंडिका’ में लिखा है कि शूरसेन (मथुरा) के लोग ‘हेराक्लीज’ (श्रीकृष्ण) के उपासक थे। मेगस्थनीज ने श्रीकृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है।
— सिकन्दर के समकालीन यूनानी लेखकों के अनुसार, पोरस की सेना अपने समक्ष हेराक्लीज (श्रीकृष्ण) की मूर्ति रखकर युद्ध करती थी।
— तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया था उसने विदिशा के बेसनगर में (शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में) विष्णु वासुदेव के सम्मान में गरूड़ ध्वज की स्थापना की तथा विष्णु स्तम्भ निर्माण करवाकर अभिलेख खुदवाया।
— मथुरा के पास मोरा नामक स्थान पर प्रथम शताब्दी का एक लेख है जिसमें ‘तोषा’ नामक एक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, प्रद्युम्न, साम्ब व अनिरूद्ध के मूर्तियों की उपासना का उल्लेख किया गया है।
— पहली शती ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में संकर्षण (बलराम) और वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। — राजा सर्वतात के दूसरी शती ईसा पूर्व के चित्तौड़गढ़ स्थित घोसुण्डी शिलालेख में वासुदेव व संकर्षण (बलराम) की पूजा का उल्लेख है।
— गुप्तकाल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त शासक ‘परमभागवत’ की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरूड़ गुप्त शासकों का राजचिह्न था।
— महाकवि कालीदास के ‘रघुवंश’ महाकाव्य में भगवान विष्णु का वर्णन कुछ इस प्रकार है— “समुद्र तल में भगवान विष्णु शेषशय्या पर लेटे पर हुए हैं, उनका पैर माता लक्ष्मी की गोद में है। उनकी चार भुजाएं हैं जिनमें क्रमश: गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए हैं एवं उनके वक्ष में कौस्तुभ नामक मणि शोभायमान है।”
— गुप्तकाल में अमरसिंह ने अपने ग्रन्थ ‘अमरकोश’ में विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है।
— गुप्तकाल में ही वाराहमिहिर ने ‘वृहत्संहिता’ में भागवत धर्म का उल्लेख किया है।
— स्कन्दगुप्त के भितरी अभिलेख में शारंगिन (कृष्ण) की पूजा के लिए कुछ गांवों को दान में दिए जाने का उल्लेख है।
— स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भगवान विष्णु की स्तुति से ही शुरू होता है। इस अभिलेख से जूनागढ़ के प्रशासक चक्रपालित द्वारा विष्णु मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है।
— स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में ही भगवान विष्णु को वामन रूप धारण करके छल से लक्ष्मी के हरण का उल्लेख मिलता है।
— दिल्ली के महरौली लौह स्तम्भ से यह जानकारी मिलती है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी।
— पृथ्वी की रक्षा करते हुए वाराह की एक विशालकाय मूर्ति का अंकन उदयगिरी पर्वत पर मिलता है जो गुप्तकालीन है।
— गुप्तकाल में ही झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनवाया गया।
— वाराह अवतार गुप्तकाल में विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार था।
— गुप्तोतर काल में भी वैष्णव धर्म भारत में प्रचलित था। अनेक राजवशों में कश्मीर के दुर्लभ वर्धन तथा ललितादित्य, बंगाल के सेन शासक, प्रतिहार नरेश देवशक्ति तथा अनेक गुहिल एवं चन्देल व चौहान नरेश भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे।
— वेंगी के पूर्वी चालुक्य भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनका राजचिह्न गुरूड़ था।
— राजपूत काल में वैष्णव धर्म का खूब प्रचार-प्रसार हुआ। भगवान विष्णु की पूजा ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय’ से की जाती थी।
— प्रतिहार शासक मिहिरभोज अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को ‘वाराह अवतार’ घोषित करता है।
— राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने ऐलारा में दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था।
— बंगाल के सेनवंशी शासक स्वयं को परम वैष्णव कहते थे।
— चन्देल शासक कीर्तिवर्मन तथा कश्मीर की महारानी ‘दिद्दा’ की मुद्राओं पर मां लक्ष्मी का चित्र उत्कीर्ण है।
— 11वीं सदी में क्षेमेन्द्र रचित ‘दशावतार चरित’ में भगवान विष्णु के दस अवतारों का वर्णन है।
— 11वीं सदी के मुस्लिम लेखक अलबरूनी ने स्थानेश्वर के निवासियों को चक्रस्वामी (विष्णु) का उपासक बताया।
— 12वीं सदी में जयदेव ने ‘गीतगोविन्द’ की रचना की।
— वैष्णव धर्म के ‘बरकरी सम्प्रदाय’ के संस्थापक का नाम नामदेव।
— वैष्णव धर्म के ‘परमार्थ सम्प्रदाय’ के संस्थापक का नाम रामदास। संत रामदास द्वारा लिखित ग्रन्थ का नाम ‘दासबोध’ है।
— वैष्णव धर्म के रामभक्त सम्प्रदाय के संस्थापक का नाम रामानन्द। रामानन्द द्वारा लिखित ग्रन्थ का नाम ‘अध्यात्म रामायण’ है।
— भारत के प्रमुख वैष्णव तीर्थस्थल - बद्रीधाम, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथद्वारा, द्वारकाधीश।
— सनातन के प्रमुख वैष्णव ग्रन्थ- विष्णुसंहिता, ईश्वर संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, पाद्मतन्त, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण।
वैष्णव धर्म (भागवत धर्म) के सिद्धान्त
भागवत सम्प्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। भागवत धर्म की मुख्य विशेषता भागवतगीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धान्त है। वायु पुराण में भागवत सम्प्रदाय के मुख्य नायकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं- 1. रोहिणी पुत्र संकर्षण (बलराम), 2. देवकी पुत्र वासुदेव, 3. रूक्मणी पुत्र प्रद्युम्न, 4. जाम्बवन्ती पुत्र साम्ब, 5. प्रद्युम्न पुत्र अनिरूद्ध।
एतरेय ब्राह्मण में भगवान विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। पतंजलि ने भी वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का नाम बताते हुए कहा गया है कि “विष्णु सर्वत्र हैं, उनमें सभी का वास है अत: वे वासुदेव हैं।” भगवान विष्णु को अपना ईष्ट देव मानने वाले उपासक वैष्णव कहलाए तथा इनसे जुड़ा धर्म वैष्णव धर्म कहलाया। वैष्णव धर्म का प्रचलन 5वीं शती ईस्वी के मध्य सर्वाधिक हुआ। भागवत धर्म के सिद्धान्तों में अवतारवाद, पंचरात्र, वीर पूजा एवं चतुर्व्यूह पूजा प्रमुख हैं।
1.अवतारवाद
‘अवतार’ शब्द प्रमुखतया भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता है। ‘अमरकोश’ एवं ‘गीतगोविन्द’ में विष्णु के अवतारों की संख्या 39 है परन्तु ‘मत्स्य पुराण’ में विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। भगवान विष्णु के दस अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं—1. मत्स्य, 2. कूर्म कच्छप, 3.वाराह, 4. नृसिंह, 5.वामन, 6. परशुराम, 7. राम, 8. बलराम, 9. बुद्ध, 10. कल्कि (भविष्य में अवतार लेंगे)।
भगवान विष्णु के 24 अवतारों का क्रम कुछ इस प्रकार है : 1. आदि पुरूष 2. चार सनतकुमार 3. वराह 4. नारद 5. नर-नारायण 6. कपिल 7. दत्तात्रेय 8. याज्ञ 9. ऋषभ 10. पृथु 11. मत्स्य 12. कच्छप 13. धनवंतरी 14. मोहिनी 15. नृसिंह 16. हयग्रीव 17. वामन 18. परशुराम 19. व्यास 20. राम 21. बलराम 22. कृष्ण 23. बुद्ध 24. कल्कि।
विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह अवतार का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ‘मत्स्य अवतार’ तथा तैतरीय ब्राह्मण में ‘वामन अवतार’ का विस्तृत उल्लेख किया गया है। नारायण, नृसिंह तथा वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं जबकि शेष सात मानवीय अवतार हैं।
अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख ‘भगवद्गीता’ में मिलता है। महाभारत महाकाव्य के ‘भीष्म पर्व’ का अंश है भगवद्गीता। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का तादात्मय विष्णु से स्थापित किया गया। महाभारत में वासुदेव कृष्ण का एक नाम ‘गोविन्द’ भी मिलता है। सूरसेन जनपद के अंधक वृष्णि संघ में जन्में कृष्ण वृष्णि संघ के प्रमुख थे। कालान्तर में पांच वृष्णि नायकों बलराम, वासुदेव कृष्ण, प्रद्युम्न, साम्ब तथा अनिरूद्ध की पूजा की जाने लगी।
2.पांचरात्र सिद्धान्त
वैष्णव धर्म का प्रधान मत पांचरात्र था। पांचरात्र मत का विकास तकरीबन तीसरी शती ईसा पूर्व में हुआ। पांचरात्र शब्द का प्रयोग नारायण के उपासकों के लिए महाभारत के ‘नारायणी प्रसंग’ में सर्वप्रथम हुआ। यहां नारायण को भी पंचरात्रिक कहा गया है। पांचरात्र सम्भवत: पांच दिन और पांच रात चलने वाला यज्ञ था।
नारद के अनुसार, रात्र का अर्थ है-ज्ञान, अत: परमतत्व, मुक्ति, युक्ति, योग तथा विषय यानि संसार इन पांच विषयों को पांचरात्र कहा गया। पांचरात्र के प्रमुख नारायण विष्णु थे।
वहीं ईश्वर संहिता के मुताबिक, भगवान ने पांच ऋषियों शाण्डिल्य, औपगायन, कौशिक, भारद्व़ाज तथा भौजायन को पांच दिन तथा पांच रात्रि तक जिस धर्म की शिक्षा दी, वह पांचरात्र धर्म है।
एक अन्य मतानुसार, पांच वृष्णिवीरों 1. वासुदेव 2. लक्ष्मी 3. संकर्षण (बलराम) 4. प्रद्युम्न 5. अनिरूद्ध (सूर्य का उपासक होने के चलते साम्ब को पांचरात्र व्यूह में शामिल नहीं किया गया) की पूजा करने के कारण इसे पंचरात्र कहा जाता है। इसमें बलि की अवधि की गणना होती थी जिसके लिए रात्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। अत: पंचरात्र का तात्पर्य उस नरबलि के अनुष्ठान से था जिसके साथ नारायण का सम्बन्ध था। कालान्तर में नरबलि प्रथा का परित्याग कर दिया गया।
3.वीरपूजा (पंचवीर )
कालान्तर में वैष्णव धर्म में वासुदेव श्रीकृष्ण के अतिरिक्त वृष्णिवंश के चार अन्य देवताओं की भी पूजा की जाने लगी। इसे वीरपूजा कहा गया तथा इन पांचों देवताओं को पंचवीर कहा गया है। वैष्णधर्म के ये पंचवीर हैं— 1. वासुदेव 2. संकर्षण 3. प्रद्युम्न 4. अनिरूद्ध 5. साम्ब।
4.चतुर्व्यूह पूजा
वासुदेव कृष्ण सहित चार वृष्णि वीरों की पूजा को चतुर्व्यूह पूजा कहा गया। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्व्यूह पूजा के चार प्रमुख देवता-
1. वासुदेव (श्रीकृष्ण)-भगवान वासुदेव में बल, विद्या, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज नामक सकल सृष्टि का बीज पौरूषी रात्रि के रूप में समाहित हैं।
2. संकर्षण (बलराम)-रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे बलराम। इनके गुण हैं- बल और विद्या। इनका कार्य है जगत की रचना करना और पंचरात्र का उपदेश देना।
3. प्रद्युम्न- कृष्ण की पत्नी रूक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का प्रमुख गुण ऐश्वर्य एवं वीर्य है। इनका कार्य सत्य मार्ग पर चलने का निर्देश देना है।
4. अनिरूद्ध- प्रद्युम्नन के पुत्र थे अनिरूद्ध। इनका गुण शक्ति और तेज है। इनका कार्य मोक्ष प्रदान करना है।
ध्यान रहे, सूर्य उपासक होने के चलते साम्ब को चतुर्व्यूह में शामिल नहीं किया गया।
दक्षिण भारत में भागवत धर्म
दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे जाते थे। अलवार अनुयायियों की भगवान विष्णु अथवा नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था थी। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का गढ़ तमिल प्रदेश था। ‘गोपी-कृष्ण’ का उल्लेख प्रारम्भिक तमिल कविताओं में प्राप्त होता है। 9वीं तथा 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण अलवारों के धार्मिक उत्थान का उत्कर्ष काल था।
दक्षिण भारत के 12 अलवार सन्तों के नाम इस प्रकार हैं— 1. पोइगई, 2. पूडम, 3. पेय, 4. पेरियालवार, 5. तिरूमलराई, 6. तिरूमंगई, 7. तिरूष्पाण, 8. तारार-अडीप-पोड़ी, 9. कुलशेखर (केरल के राजा), 10. नम्मालवार, 11. मधुरकवि, 12. आंडाल (एकमात्र महिला अलवार)।
दक्षिण के भक्ति आन्दोलन में निहित प्रमुख 12 अलवार सन्तों में तिरूमंगाई, पेरिय अलवार, महिला संत अण्डाल तथा नाम्मालवार का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महिला संत अण्डाल ने खुद को विष्णु की प्रेमिका माना।
नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने विष्णु को सगुण तथा निर्गुण दोनों रूप में स्वीकार किया है। मिहिर भोज ने विष्णु को ‘हृषीकेश’ कहा है।
केरल का सन्त राजा कुलशेखर भी भगवान विष्णु का भक्त था। राजा कुलशेखर की भगवान श्रीराम में भी अगाध आस्था थी। राजा कुलशेखर ने ‘पेरूमल तिरूमोलि’ नामक ग्रन्थ की रचना की। दक्कन के अलवारों में भगवान वामन की पूजा चिरकाल तक होती रही। दक्कन के अलवार लोग वाराह की भी उपासना करते थे।
अलवार संतों के बाद आचार्यों ने वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया। जहां अलवार संतों ने वैष्णव धर्म के भावनात्मक पक्ष का प्रसार किया वहीं आचार्यों ने इसके बौद्धिक और दार्शनिक पक्ष को अपनाया। आचार्यों ने कर्म, ज्ञान और भक्ति के सम्मिश्रण से वेद, उपनिषद, गीता और तमिल प्रबन्धम के बीच सामन्जस्य स्थापित किया।
आचार्यों को ही ‘आधुनिक वैष्णव धर्म’ का निर्माता माना जाता है। इन आचार्यों में सर्वप्रथम नाथमुनि थे। आचार्य नाथमुनि को राजेन्द्र चोल का समकालीन माना जाता है। राजेन्द्र चोल ने तमिल ‘प्रबन्धम’ को वेद का स्थान दिया और श्रीरंगम के मंदिर में प्रबन्धम के पाठ का श्रीगणेश करवाया। इसका अनुसरण सभी वैष्णव मंदिरों में किया गया।
वैष्णव धर्म के प्रमुख सम्प्रदाय, मत तथा संस्थापक आचार्य
- वैष्णव सम्प्रदाय — विशिष्टाद्वैत — रामानुज (12वीं शताब्दी)
- ब्रह्म सम्प्रदाय — द्वैतवाद — माधव (13वीं शताब्दी)
- रूद्र सम्प्रदाय — शुद्धाद्वैत— वल्लभाचार्य (13वीं शताब्दी)
- सनक सम्प्रदाय — द्वैताद्वैत— निम्बार्क (13वीं शताब्दी)