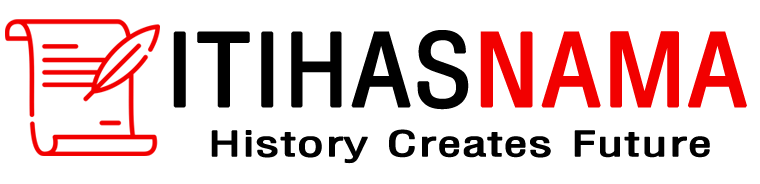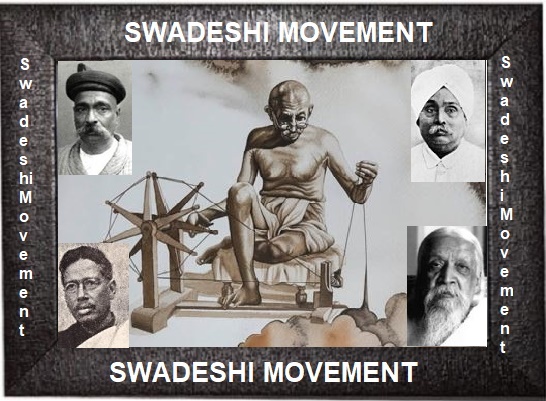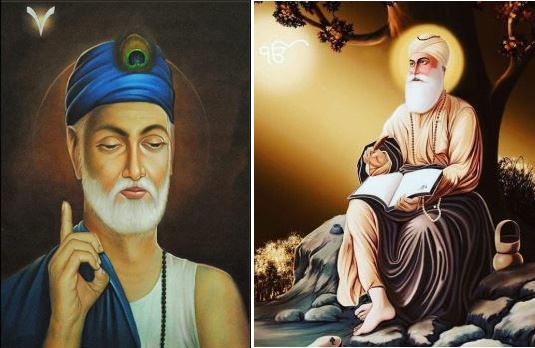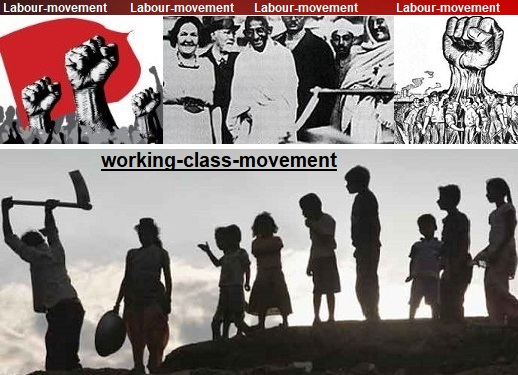
19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में मजदूर संघ की गतिविधियां शुरू हुईं। रेलवे का निर्माण इस दिशा में प्रथम कदम था। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराईयां व्याप्त थीं, जैसे- काम के अधिक घंटे, आवास की असुविधा, कम वेतन, अत्यधिक असुरक्षा आदि। कारखानों में सुधार हेतु प्रथम प्रयास समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया।
1870 ई. में बंगाल के शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब ‘श्रमजीवी समिति’ स्थापित किया और ‘भारत श्रमजीवी’ नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। साल 1877 में नागपुर स्थित एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने अपने वेतन दरों के विरूद्ध हड़ताल का आयोजन किया। 1878 ई. में सोराबजी शपूरजी बंगाली ने बम्बई विधानसभा में श्रमिकों की कार्यविधि से जुड़ा एक विधेयक पेश करना चाहा लेकिन असफल रहे।
साल 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे (N.M.Lokhande) ने ‘बम्बई मिल हैन्डस एसोसिएशन’ की स्थापना की। इसे भारत का पहला मजदूर संघ माना जा सकता है। लोखण्डे ने 1880 ई. में अंग्रेजी तथा मराठी में ‘दीनबन्धु’ नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया।
प्रारम्भिक मजदूर आन्दोलन से जुड़ने वाली संस्थाओं में ‘भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी’ (1897 ई.), ‘कलकत्ता मुद्रक संघ’ (1905 ई.), ‘कामगार हितवर्धक सभा’ (1909 ई.), ‘सामाजिक सेवा संघ’ (1911 ई.) आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है।
शुरूआती दिनों में देश के राष्ट्रवादी नेताओं का रूख मजदूर आन्दोलन के प्रति उदासीनता का था। इसका मुख्य कारण साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन था जो अपने प्रथम चरण में था। राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन्हीं मुद्दों से लड़ना चाहते थे जिसमें समूचे देश की भागीदारी हो।
देश के प्रारम्भिक राष्ट्रवादी नेताओं ने ‘कारखाना अधिनियमों -1881 व 1891 ई.’ की आलोचना की क्योंकि वे श्रम कानूनों को औद्योगीकरण के मार्ग में बाधक नहीं बनने देना चाहते थे। राष्ट्रवादियों को इस बात की आशंका थी कि सरकार इन अधिनियमों के तहत ब्रिटिश उत्पादों को बढ़ावा देकर भारतीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक के अखबार ‘मराठा’ ने मिल मजदूरों के अधिकारों तथा रियायतों के बारे में लिखना शुरू किया।
मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल साल 1899 में ‘ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर रेलवे’ के मजदूरों द्वारा कम वेतन एवं अधिक कार्यावधि के कारण की गई थी। 7 अगस्त 1905 ई. को कलकत्ता के टाउन हॉल में ‘स्वदेशी आन्दोलन’ की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 ई. को बंगाल विभाजन के दिन मजदूरों ने समूचे बंगाल में हड़ताल रखी। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय ‘आमार सोनार बांग्ला’ नामक गीत लिखा जो 1971 ई.में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना।
साल 1908 में बाल गंगाधर तिलक को आठ वर्ष की सजा होने पर बम्बई के कपड़ा मजदूर तकरीबन एक सप्ताह तक हड़ताल पर रहे। यह उस समय मजदूरों की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी। साल 1917 में हुई रूसी क्रांति के बाद भारत में मजदूर आन्दोलनों की वास्तविक शुरूआत हुई।
अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी आन्दोलन के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए ‘स्वदेशी बान्धव समिति’ की स्थापना की। वी.आर.नारे, एस.के.बोले तथा एन.ए. तालेकेरकर ने ‘बम्बई कामगार हितवर्धिनी सभा’ की स्थापना की। वी.पी.वाडिया द्वारा साल 1918 में स्थापित ‘मद्रास मजदूर संघ’ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। वास्तव में ‘मद्रास मजदूर संघ’ की स्थापना जी. रामनजुलू नायडू और जी. चेल्लापति चेट्टी ने की थी और वी.पी.वाडिया इस यूनियन के अध्यक्ष थे।
एनी बेसेन्ट के सहयोगी वी.पी. वाडिया ने 1919 ई. में इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन तथा एन.एम.जोशी ने 1920 ई. में इसी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1918 में महात्मा गांधी ने ‘अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन’ की स्थापना की जो सम्भवत: उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। 1919 ई. में बंगाल में जूट श्रमिक संघों ने पहली बड़ी हड़ताल की।
31 अक्टूबर 1920 ई. को नारायण मल्हार जोशी ने ‘अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ (एटक) की स्थापना की। एटक का पहला सम्मेलन 1920 ई. में बम्बई में हुआ जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा थे जबकि महामंत्री दीवान चमन लाल थे। 1920 ई. में महात्मा गांधी ने ‘मजदूर महाजन संघ’ की स्थापना की।
1922 ई. के गया अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने एटक के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। एटक यानि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस नेताओं के नाम इस प्रकार हैं- लाला लाजपत राय (1920 ई.), चितरंजन दास, सी.एफ.एन्ड्रूज, जितेन्द्र मोहन सेन गुप्त, जवाहरलाल नेहरू (1929 ई.), सुभाषचन्द्र बोस (1931 ई.), सरोजिनी नायडू तथा सत्यमूर्ति।
यद्यपि साल 1926-27 के दौरान एटक में दो गुट बन गए—1. सुधारवादी गुट 2. क्रांतिकारी गुट। एटक के क्रांतिकारी गुट ने स्वयं को मास्को स्थित तीसरे इन्टरनेशनल से संलग्न किया। वहीं एन.एम.जोशी के नेतृत्व में सुधारवादी गुट एम्सटर्डम स्थित अन्तरराष्ट्रीय फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन से संलग्न होना चाहता था।
एटक पर वामपंथी विचारधारा हावी होने के कारण साल 1929 में एन.एम.जोशी के नेतृत्व में एटक का विभाजन हो गया। परिणामस्वरूप एन.एम.जोशी के नेतृत्व में वी.वी.गिरी की अध्यक्षता व मृणालकांति बोस के सहयोग से ‘अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन’ की स्थापना हुई।
कम्यूनिस्ट लीडर देशपांडे ने 1929 ई. में ‘लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ की स्थापना की। बम्बई में साम्यवादियों के मिल मजदूर संगठन का नाम ‘गिरनी कामगार यूनियन’ था। 1928 ई. में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लम्बी हड़ताल का आयोजन किया गया।
साल 1929 से 1939 ई. के दौरान मजदूर संगठनों में फूट के कारण अनेक ट्रेड यूनियनों का जन्म हुआ। इस फूट के चलते मजदूर आन्दोलन की प्रगति में बाधा आई। 1926 ई. में प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ जिसमें ट्रेड यूनियन बनाने व हड़ताल करने को कानूनी मान्यता तो अवश्य मिली परन्तु मजदूरों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई।
घनश्यामदास बिड़ला तथा पुरूषोत्तम दास ठाकुरदास के प्रयासों से साल 1927 में एफआईसीसीआई (FICCI) की स्थापना हुई। 1929 ई. में व्यापार विवाद अधिनियम पारित किया गया जिसमें औद्योगिक झगड़ों के निपटारे के लिए प्रबन्ध तंत्र को मनमानी शक्ति दी गई।
कांग्रेस के वामपंथी नेताओं में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरन चन्द्र जोशी और सोहन सिंह जोश ने ‘कामगार किसान पार्टी’ की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय कांग्रेस ने नारा दिया कि “मजदूर और किसान कांग्रेस हाथ-पांव हैं।”
भारत सरकार अधिनियम-1935 के तहत मजदूर संघों तथा श्रमिक निर्वाचन मंडलों के माध्यम से श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। 1937-39 ई. के चुनावों में विभिन्न प्रान्तों बनी कांग्रेस सरकारों के सहयोग से मजदूर आन्दोलन ने एकबार फिर से जोर पकड़ा। 1937 ई. के चुनावों के बाद सरकार ने कानपुर में श्रमिकों की हड़ताल की जांच के लिए राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में कानपुर श्रमिक जांच समिति नियुक्त की।
द्वितीय विश्वयुद्ध (3 सितम्बर ,1939 ई.) के विरोध में बम्बई के मजदूरों ने 2 अक्टूबर 1939 ई. को विश्व हड़ताल का आयोजन किया जिसमें तकरीबन 90 हजार मजदूरों ने हिस्सा लिया। मानवेन्द्र नाथ राय ने (M.N.Rai) ‘अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ यानि एटक से अलग होकर 1 नवम्बर 1941 ई. को ‘भारतीय श्रमिक परिसंघ’ (इंडियन फेडरेशन आफ लेबर) की स्थापना की।
भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 9 अगस्त, 1942 ई. को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिए जाने पर देश के प्रमुख शहरों- दिल्ली, कलकत्ता, लखनउ, कानपुर, बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, मद्रास, इन्दौर, बंगलौर आदि में श्रमिक हड़तालें हुईं।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम वर्षों (1946-47 ई.) में पूरे देश में श्रमिक हड़तालें हुईं, इनमें सबसे प्रसिद्ध हड़ताल जुलाई 1946 ई. में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल थी। अगस्त 1946 ई. में दक्षिण भारत के रेल मजदूरों ने हड़ताल की। मई, 1947 में एटक से अलग होकर सरदार वल्लभभाई पटेल ने ‘भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ (INTUC) का गठन किया। वहीं कांग्रेस के समाजवादी गुट ने ‘हिन्द मजदूर सभा’ की स्थापना की।
आजादी के बाद भारत में मजदूर आन्दोलन
आजादी के बाद देश में बीएमएस यानि भारतीय मज़दूर संघ तथा सीटू (भारतीय ट्रेड यूनियनों का केन्द्र) जैसे कई ट्रेड यूनियनें अपने अस्तित्व में आईं। बता दें कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने एटक से अलग होकर सीटू का गठन किया था।
आजादी के दिनों में ट्रेड यूनियन से जुड़े कई कानून पास किए गए जैसे- औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और श्रम संबंध विधेयक तथा ट्रेड यूनियन बिल-1949। साल 1947 से 1960 के बीच मजदूर वर्ग के हालातों में सुधार होने से हड़तालों की संख्या में गिरावट देखने को मिला।
साल 1991 में उदारीकरण, निजीकरण अथवा वैश्वीकरण की शुरूआत हुई जिसने पूंजी के मुकाबले श्रमिकों के महत्व को कमतर कर दिया। श्रमिकों के लिए कोई भी वैधानिक मजदूरी सुनिश्चित नहीं की गई। यहां तक कि नियोक्ताओं को भाड़े तथा नौकरी से निकालने का पूरा अधिकार दिया गया।
मजदूर आन्दोलन की कमजोरियां - आजादी के बाद ट्रेड यूनियनों की बहुलता, मजदूरों के सभी वर्गों का शामिल नहीं होना, अधिकांश ट्रेड यूनियनों का मजदूरों की समस्याओं के प्रति अनुत्तरदायी होना, राजनीतिक चेतना के आभाव में मजदूरों के बीच फूट, महिला श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के समस्याओं की अनदेखी के चलते मजदूर आन्दोलन कमजोर हुआ।
मजदूर आन्दोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
— साल 1854 में एक स्कॉटिश उद्यमी द्वारा कलकत्ता में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी।
— 19वीं सदी के अंत में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के अतिरिक्त अहमदाबाद, कानपुर, सोलापुर और नागपुर जैसे शहरों में कारखाने स्थापित किए गए।
— ट्रेड यूनियनों के गठन से पूर्व चाय - नील बागान व खदान श्रमिकों तथा कपास और जूट उद्योग के श्रमिकों ने आन्दोलन किए।
— ब्रह्म समाज ने श्रमिकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बंगाल में 1878 ई. में ‘वर्किंग मेन्स मिशन’ का गठन किया।
— साल 1920 में सोवियत संघ में गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) गठन के तुरंत बाद ही श्रमिक आंदोलनों में सक्रिय हो गई।
— होमरूल आंदोलन और असहयोग आंदोलन (1915-1922) के साथ-साथ श्रमिक आंदोलन का भी पुनरुत्थान हुआ।
— ट्रेड यूनियन अधिनियम -1926 के तहत ट्रेड यूनियनों को कानूनी संघ में रूप में मान्यता मिली।
— साल 1927 में पंजाब में मजदूर और किसान पार्टी बनी। उर्दू साप्ताहिक ‘मेहनतकश’ इसका मुख पत्र था।
— साल 1928 में मद्रास में भी एक मजदूर और किसान पार्टी बनी। इस पार्टी क्रॉन्फ्रेस में ब्रिटिश कम्यूनिस्ट फिलिप स्प्राट ने भाग लिया।
— लाजपत राय ने कहा- “साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वां बच्चे हैं।”
— भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना 1925-26 ई. में बंगाल में ‘लेबर स्वराज पार्टी’ के नाम से की गई।
— लेबर स्वराज पार्टी के संस्थापक थे- मुजफ्फर अहमद, नजरूल इस्लाम, कुतुबुद्दीन अहमद तथा हेमन्त कुमार। कालान्तर में लेबर स्वराज पार्टी का नाम बदलकर बंगाल कृषक और श्रमिक दल रख दिया गया। ‘लांगल’ इस पार्टी का मुख पत्र था।
— बम्बई में ढुंडिराज ठेंगड़ी (अध्यक्ष) तथा एस. मिरजकर (सचिव) ने साल 1927 में बम्बई मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की। मराठी में साप्ताहिक अखबार ‘क्रांति’ इस पार्टी का मुख पत्र था।
— नवम्बर 1928 ई. में फिलिप स्प्रेट, मुजफ्फर अहमद, अब्दुल मजीद, सोहन सिंह जोश तथा पूरन चन्द्र जोशी ने यू.पी. किसान पार्टी की स्थापना की। पी.सी.जोशी इसके सचिव थे।
— 1927 ई. में भारत में पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया।
— 1 मई को पूरे विश्व में मजदूर दिवस उन मजदूरों की याद में मनाया जाता है, जिनकी 1 मई, 1861 ई. को अमेरिका में पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी।
— 1928 ई. में सभी मजदूर पार्टियों ने मिलकर ‘अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी’ का गठन किया। जिसका पहला अधिवेशन दिसम्बर, 1928 में कलकत्ता में सोहन सिंह जोश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।
— 1928 ई. में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लम्बी हड़ताल का आयोजन किया गया।