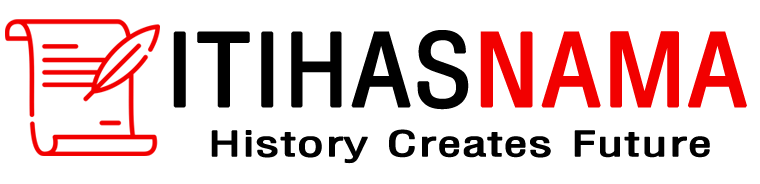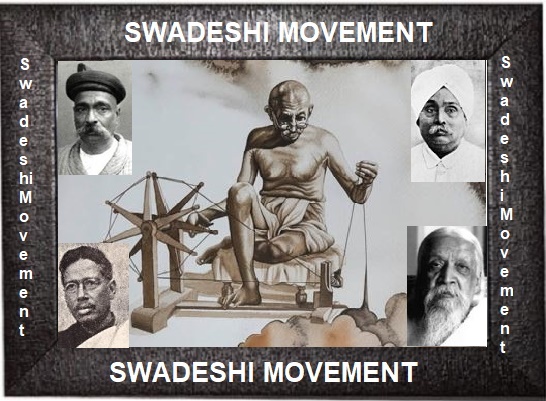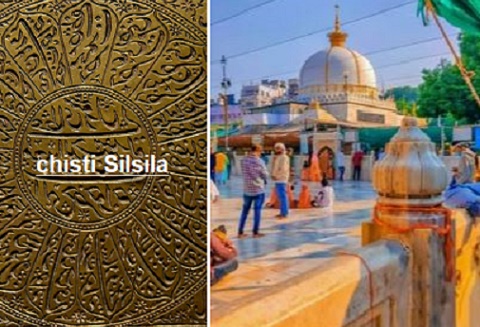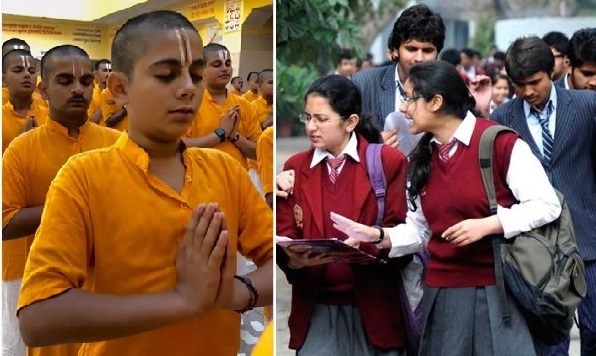
प्राचीन काल में गुरुकुल, आश्रम एवं बौद्ध मठ शिक्षा ग्रहण के प्रमुख केन्द्र थे। नालन्दा, तक्षशिला एवं वल्लभी प्राचीन भारत के विख्यात विश्वविद्यालय थे। 18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के केन्द्र लुप्तप्राय हो गए। देश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही विद्या से विमुख होने लगे। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने शासन के शुरूआती दिनों भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु कोई प्रयास नहीं किया। इन दिनों कुछ उदार अंग्रेजों, ईसाई मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में सार्थक प्रयास किया।
भारतवासी ऐसी शिक्षा चाहते थे जो उन्हें जीविकोपार्जन में मदद कर सके। वहीं ईस्ट इंडिया कम्पनी को अपना प्रशासन चलाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो स्थानीय भाषाओं के ज्ञाता हों। यही वजह है कि राजा राममोहन राय ने कलकत्ता, बनारस आदि शहरों में मदरसे तथा संस्कृत कॉलेजों के स्थापना के सरकारी प्रयत्नों की कड़ी आलोचना की।
ईसाई मिशनरियों का योगदान
1. भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार का मुख्य कार्य ईसाई मिशनरियों द्वारा शुरू किया गया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना था।
2. ईसाई मिशनरियों ने बंगाल स्थित सेरामपुर (श्रीरामपुर) को भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार का मुख्य केन्द्र बनाया तथा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया।
3. सेरामपुर मिशनरी का निर्माण 1799 ई. में डॉ. केरे, मार्शमैन तथा वार्ड ने मिलकर किया था।
4. सेरामपुर की ईसाई मिशनरियों ने साल 1818 में ‘बैपटिस्ट मिशन कॉलेज’ की स्थापना की।
5. ईस्ट इंडिया कम्पनी ने साल 1813 में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास शुरू किया।
6. चार्टर एक्ट-1813 के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वह भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा साहित्य में सुधार के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपए खर्च करे।
7. मद्रास में मिशनरियों का शिक्षा प्रसार सबसे अधिक था।
8. उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में शिक्षा की देशी पद्धति को मुख्य स्थान प्राप्त था तत्पश्चात देशी पद्धति को हटाकर उसकी जगह आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास किया गया।
9. नई शिक्षा पद्धति का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था।
10. राजा राममोहन राय ने कलकत्ता के सूरीपाड़ा में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला।
11. साल 1822 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में कार्नवालिस स्क्वायर के पास ‘एंग्लो हिन्दू कॉलेज’ की स्थापना की।
12. साल 1817 में डेविड हेयर तथा राजा राममोहन राय आदि विद्वानों ने मिलकर कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में ‘प्रेसिडेन्सी कॉलेज’ बना।
13. जे.ई.डी. बेथून ने 1849 ई. में भारतीय बालिकाओं के लिए एक विद्यालय स्थापित किया।
14. लार्ड डलहौजी ने ‘बेथून महाविद्यालय’ को भारतीय महिला शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बना दिया।
पाश्चात्य विद्वानों की भारतीय शिक्षा में रूचि
— गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अरबी तथा फारसी भाषा के अध्ययन के लिए साल 1781 में ‘कलकत्ता मदरसा’ की स्थापना की।
— विलियम जोन्स ने 1784 ई. में ‘एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल’ की स्थापना की।
— ब्रिटिश रेजिडेन्ट जोनाथन डंकन ने 1791 ई. में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की।
— मिसेज एनी बेसेन्ट ने बनारस में 1898 ई. में सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना की।
— सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज साल 1916 में बनारस हिन्दू विश्विद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जिसके संस्थापक मदनमोहन मालवीय थे।
— 1800 ई. में लॉर्ड वेलेजली ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए ‘फोर्ट विलियम कॉलेज’ की स्थापना की।
— डेविड हेयर ने 1820 ई. में कलकत्ता में ‘बिशप कॉलेज’ की स्थापना की।
आंग्ल-प्राच्य विद्या विवाद
लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 10 सदस्य थे, जो शिक्षा के माध्यम को लेकर दो दलों में विभाजित थे। इसमें से एक दल प्राच्य विद्या का समर्थक था, जिसके नेता लोक शिक्षा समिति के सचिव एच.टी. प्रिंसेप थे। वहीं दूसरा दल पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था जिसका नेतृत्व मद्रास के गवर्नर टामस मुनरो तथा बम्बई के गवर्नर एलफिन्स्टन कर रहे थे, जिसका समर्थन कालान्तर में लॉर्ड मैकाले ने भी किया।
प्राच्य विद्या के समर्थक चाहते थे कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन मिले तथा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का इन्ही भाषाओं में प्रसार किया जाए। इस प्रकार दोनों दलों के गतिरोध को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया। लार्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना एक लेख (Macaulay minute) प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय भाषा साहित्य की तीखी आलोचना की गई। मैकाले के अनुसार, “यूरोपीय पुस्तकालय की एक आलमारी भारत तथा अरब के सम्पूर्ण साहित्य के बराबर मूल्यवान है।”
पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक लॉर्ड मैकाले एक ऐसा समूह तैयार करना चाहता था “जो रूप-रंग से भारतीय हों किन्तु विचारों, रूचि और बुद्धि में अंग्रेज हों।” इस प्रकार साल 1835 में अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया।
शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धान्त
शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धान्त से तात्पर्य है “शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए।” ऐसे में उच्च वर्ग के शिक्षित होने पर छन-छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धान्त का प्रतिपादन लॉर्ड आकलैण्ड ने किया था किन्तु लॉर्ड मैकाले ने इस सिद्धान्त पर पहले भी कार्य किया था।
साल 1854 से पूर्व शिक्षा का विकास
संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर जेम्स टॉमसन (1843 से 1854 ई.) ने देशी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई जिसके अनुसार, छोटे-छोटे अंग्रेजी स्कूलों को बन्द कर दिया गया तथा अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक सीमित कर दी गई। गांवों में गणित तथा कृषि विज्ञान जैसे विषयों को स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया।
लार्ड हर्डिंग ने 1847 ई. में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना की। 1847 ई. में ही थामसन ने रूड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की।1849 ई. में पंजाब में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अमृतसर तथा लाहौर में स्कूल खोले गए।
तत्पश्चात 1851 ई. में ‘पूना संस्कृत कॉलेज’ तथा ‘पूना अंग्रेजी स्कूल’ को मर्ज कर ‘पूना कॉलेज’ बनाया गया। 1852 ई. में आगरा में ‘सेंट जॉन्स कॉलेज’ की स्थापना हुई। 1854 ई. में बम्बई में ‘ग्रांट मेडिकल कॉलेज’ की नींव डाली गई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1847 ई. से पूर्व भारत में कुल 19 विश्वविद्यालय थे।
1854 ई. का चार्ल्स वुड डिस्पैच
साल 1854 में ब्रिटेन की अर्ल ऑफ एबरडीन की मिली जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड को भारतीयों की भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना बनाने का दायित्व सौंपा गया।
इस सम्बन्ध में सर चार्ल्स वुड ने जो सिफारिशें (चार्ल्स वुड डिस्पैच) प्रस्तुत की, उसे ‘भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा’ कहा गया। वुड घोषणापत्र के आधार पर 1855 ई.में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई तथा लन्दन विश्वविद्यालय के आधार पर 1857 ई. में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक-एक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।
चार्ल्स वुड डिस्पैच में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत में पाश्चात्य कला, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान एवं साहित्य का प्रसार करे। देशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले किन्तु उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। गांवों में देशी भाषा में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं तथा जिलास्तर पर एंग्लों वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाएं।
व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। शिक्षा में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाए।
हंटर शिक्षा आयोग (1882-1883 ई.)
साल 1882 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने वुड घोषणापत्र की समीक्षा के लिए डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। हंटर आयोग में 20 सदस्य थे, जिनमें से 8 सदस्य भारतीय थे। इस आयोग का मुख्य काम प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था।
हंटर आयोग ने देश के सभी प्रान्तों का भ्रमण किया और तकरीबन 200 प्रस्ताव पारित किए। हंटर आयोग के सुक्षाव पर प्रान्तीय सरकारों ने कार्य किया और अगले 20 वर्षों तक माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हंटर आयोग के सुक्षाव के बाद 1882 में पंजाब तथा 1887 ई.में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904
लार्ड कर्जन ने सितम्बर 1901 में शिमला में उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें उसने मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना की। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को ‘शिमला प्रस्ताव’ के नाम से जाना जाता है। 1902 में कर्जन ने सर टॉमर रैले की अध्यक्षता में एक ‘विश्वविद्यालय आयोग’ की स्थापना की। रैले कमीशन में में सैय्यद हुसैन बिलग्रामी (हैदराबाद के निजाम का लोक शिक्षा विभाग का निदेशक) तथा जस्टिस गुरूदास बनर्जी (कलकत्ता हाईकोर्ट का जज) भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे।
रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में ‘भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम’ पारित किया गया। ‘भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम’ की सिफारिशें कुछ इस प्रकार थीं —
— विश्वविद्यालयों में शोध कार्य तथा अध्ययन के लिए आचार्यों तथा प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए।
— विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
— पुराने विश्वविद्यालयों में सरकार द्वारा चयनित उपसदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 होनी चाहिए। उपसदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो। इस प्रकार विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया।
— अंग्रेजी सरकार ने 12 फरवरी 1913 ई. को निरक्षरता समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रान्तीय सरकारों को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का निर्देश दिया तथा प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया।
सैडलर आयोग 1917-19
1917 ई. में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर डॉ. एम. ई. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। सैडलर आयोग के सदस्यों में दो भारतीय भी थे, जिनमें से एक का नाम सर आशुतोष मुखर्जी तथा दूसरे का नाम डॉ. जियाउद्दीन अहमद था।
सैडलर आयोग का कहना था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना अति आवश्यक है। सैडलर आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं —
— 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश।
— विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए ‘माध्यमिक शिक्षा बोर्ड’ का गठन।
— स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो।
— महिला शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर।
— अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा पर विशेष ध्यान।
— प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति की नियुक्ति का सुझाव।
— साल 1916 से 1921 के बीच मैसूर (1916), बनारस (1916), पटना (1917), ढाका, अलीगढ़ (1918), लखनऊ (1921), हैदराबाद तथा नागपुर (1923) आगरा (1927), आंध्र (1926) और अन्नामलाई (1926) में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।
विशेष : साल 1919 में मौंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद शिक्षा प्रान्तीय विषय बन गया। शिक्षा के लिए केन्द्रीय अनुदान बन्द कर दिया गया।
हार्टोग समिति 1929
शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट को रोकने हेतु 1929 ई. में भारतीय परिनियत आयोग (India Statutory commission) ने सर फिलिप होर्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की, जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। होर्टोग समिति की सिफारिशें कुछ इस प्रकार थीं —
— प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की आलोचना की गई।
— ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिल स्कूल के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश की जगह व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाए।
— विश्वविद्यालयी शिक्षा के विषय में यह सुझाव दिया गया कि जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के योग्य हैं, केवल उन्हें ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाए।
वर्धा योजना
साल 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र ‘द हरिजन’ में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे ‘वर्धा योजना’ की संज्ञा दी गई।
— जाकिर हुसैन समिति ने शिक्षा योजना के साथ ही कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए।
— वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धान्त हस्त उत्पादक कार्य था, जिससे शिक्षकों के वेतन का भी प्रबन्ध हो जाता था। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा में 7 वर्षों तक अध्ययन करना था।
— द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने तथा मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने से वर्धा योजना लागू नहीं की जा सकी।
सार्जेन्ट योजना 1944
साल 1944 में ब्रिटिश भारत के शिक्षा सलाहकार जान सार्जेन्ट ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित थीं —
— देश में प्रारम्भिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं।
— विद्याविषयक - प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए दो प्रकार के विद्यालय हों।
— 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा।
— 11 से 17 वर्ष की उम्र तक अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था।
— सार्जेन्ट योजना के तहत 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था। बाद में खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर 16 वर्ष कर दिया।
नोट — सार्जेन्ट योजना के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया।
राधाकृष्णन आयोग 1948-1949
भारत सरकार ने नवम्बर 1948 में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं —
— विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन।
— विश्वविद्यालयों की परीक्षा तिथि से पूर्व 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए।
— उच्च शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य- सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए।
— प्रशासनिक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि अनिवार्य नहीं।
— शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए।
— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देशभर में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (university grants commission)
राधाकृष्णन आयोग के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए 1953 ई. में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के अधिनियम के अनुसार एक स्वायत्ततापूर्ण परिनियत पद (Autonomous statutory status) दे दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार करती है।
कोठारी शिक्षा आयोग 1964-1966 ई.
जुलाई 1964 में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा बनाने के लिए इंग्लैण्ड, अमेरिका, रूस आदि से प्रमुख शिक्षाशास्त्री तथा वैज्ञानिक इस आयोग से सम्बद्ध किए गए। इसके बाद कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए —
— शिक्षा के सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से समाज सेवा (Social Service) और कार्य अनुभव (Work Experience) से जुड़ी सामान्य शिक्षा आरम्भ किए जाने चाहिए।
— नैतिक शिक्षा (Moral Education) तथा सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibility) की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया गया।
— माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए।
— बड़े विश्वविद्यालयों में एक छोटी सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम अर्न्तराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे।
— विद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा क्वालिटी पर विशेष बल दिया जाए।
— शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि, कृषि में अनुसन्धान तथा इससे सम्बन्धित विज्ञान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ई.
कोठारी आयोग को आधार बनाकर भारत सरकार ने 1968 ई. में राष्ट्रीय शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित तत्वों पर बल दिया गया था —
— चौदह वर्ष की उम्र तक अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा।
— अध्यापकों के लिए पद तथा वेतन में वृद्धि।
— तीन भाषाई फार्मूले को स्वीकार करना और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास।
— विज्ञान तथा अनुसन्धान की शिक्षा का समानीकरण।
— कृषि तथा उद्योग के लिए शिक्षा का विकास।
— पाठ्य पुस्तकों की उत्तमता के साथ सस्ती पुस्तकों का उत्पादन।
— राष्ट्रीय आय का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करना।
भारत में शिक्षा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
1. गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था — चार्ल्स विल्किन्स।
2. चार्ल्स विल्किन्स द्वारा अंग्रेजी अनुवादित ‘गीता’ की प्रस्तावना किसने लिखी थी — वारेन हेस्टिंग्ज।
3. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मुख्य कार्य — प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की खोज एवं अध्ययन।
4. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का वर्तमान नाम — रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल।
5. भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक — चार्ल्स ग्रान्ट।
6. साल 1835 में लार्ड मैकाले ने एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया — मैकाले मिनट।
7. साल 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने डाली — लॉर्ड विलियम बेंटिक।
8. बाल गंगाधर तिलक और उनके साथियों ने साल 1870 में पूना में किस कॉलेज की स्थापना की — फर्ग्यूसन कॉलेज।
9. आर्यसमाज द्वारा 1886 ई. में लाहौर में कौन सा कॉलेज खोला गया — दयानंद ऐंग्लो वैदिक कॉलेज।
10. साल 1848 में लड़कियों के लिए भारत का पहला प्राथमिक विद्यालय किसने खोला — जोतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने।
11. शिक्षा के ‘अधोमुखी निस्यंदन सिद्धान्त’ का प्रतिपादन किसने किया — लार्ड आकलैण्ड।
12. शिक्षा का अधोमुखी सिद्धान्त क्या है — ‘सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए’।
13. चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है — भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा।
14. ब्रिटिश भारत में पहला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ — कलकत्ता में।
15. लार्ड कर्जन के समय भारत का प्रथम शिक्षा महानिदेशक — एच. डब्ल्यू आरेन्ज।
16. किस गवर्नर जनरल के समय 1904 ई. में प्राचीन स्मारक, अभिलेख संरक्षण अधिनियम पारित किया गया — लार्ड कर्जन।
17.ब्रिटिश भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई — 1910 ई. में।
18. दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई — 1922 ई. में।
19. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी — 1916 ई.।
20. गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू प्रमुख शिक्षा आयोग
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी — चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ई. ।
गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन — हन्टर शिक्षा आयोग 1882-1883 ई. ।
गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड — सैडलर आयोग 1917-1918 ई. ।
गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन — हार्टोग समिति 1929 ई. ।
गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल — सार्जेण्ट योजना 1944 ई. ।
गवर्नर जनरल लॉर्ड माउण्ट बेटन — राधाकृष्णन आयोग 1948 ई. ।