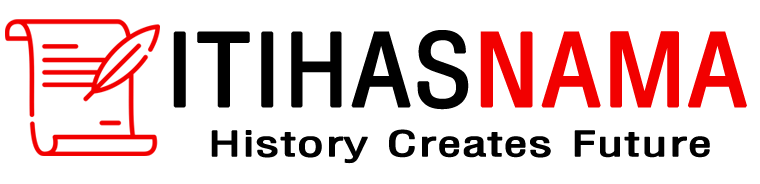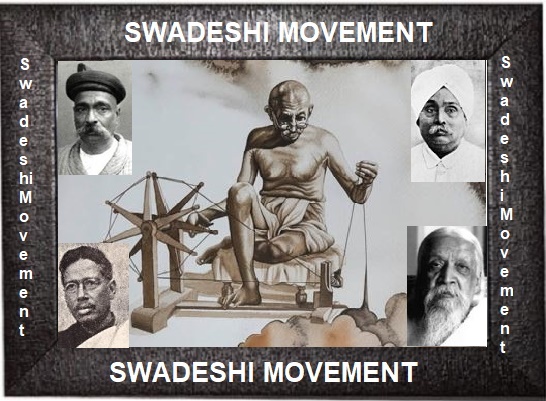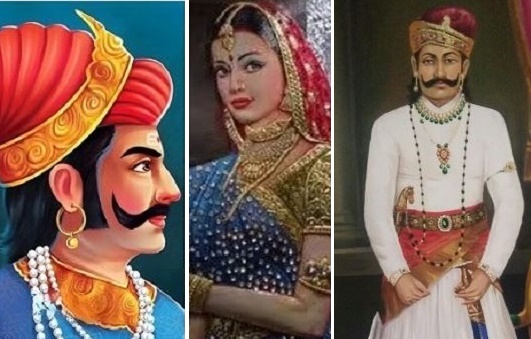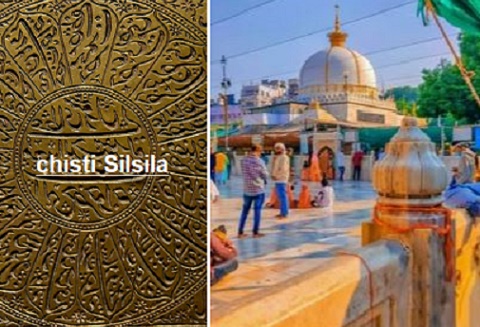19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20 शताब्दी के पहले दशक में भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह काल भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान का काल कहा जाता है। हांलाकि ज्यादातर अंग्रेजी लेखकों ने भारत में अंग्रेजी राज को ही राष्ट्रीय भावना के उदय के लिए श्रेय दिया है।
आर. कूपलैंड ने लिखा है कि “भारतीय राष्ट्रीयवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी।” रैम्जे मैकडोनाल्ड ने कहा कि “भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। भारत का वर्तमान बौद्धिक एवं नैतिक हलचल हमारे कार्य की निन्दा नहीं अपितु प्रशंसा की बात है।”
हांलाकि आर. कूपलैंड यह कहना भूल गए कि अंग्रेजी राज ने तो शुरू से ही भारतीय राष्ट्रवाद का गला घोंटने का प्रयास किया। ऐसे में यह कहना लाजिमी होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद कुछ अंश में समूचे संसार में उभरते हुए राष्ट्रवाद तथा आत्मनिर्णय की भावना का परिणाम था। बावजूद इसके ऐसे 14 तत्व प्रमुख हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में भरपूर सहायता की।
1. सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों की भूमिका
भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डॉ. आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, आर. जी. भंडारकर तथा केशव चन्द्र सेन जैसे सुधारवादियों ने भारतीयों के अन्तर्मन को झकझोर दिया।
ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन आदि अस्तित्व में आए, जिससे हिन्दू धर्म में सुधार हुआ। उसी प्रकार से मुसलमानों, सिक्खों तथा पारसियों में भी सुधारवादी संस्थाएं बनीं।
धार्मिक क्षेत्र में हुए सुधार अन्दोलनों ने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद तथा वंशानुगत पुरोहित पद्धति को चुनौती दी। समाजिक क्षेत्र में इन्होंने जाति प्रथा, छूआछूत तथा अन्य सामाजिक तथा वैधानिक असमानताओं को चुनौती दी। इन सभी सामाजिक आन्दोलनों का गठन प्रजातंत्र, सामाजिक समानता, तर्क, बुद्धिवाद तथा उदारवादी विचारों के आधार पर हुआ था।
हांलाकि धार्मिक संगठनों में से अधिकतर का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, किन्तु जो लोग इनके प्रभाव में आए उनमें शीघ्र ही आत्मसम्मान एवं देशभक्ति की भावनाएं विकसित हो जाती थीं। चूंकि ज्यादातर सुधारवादी संस्थाएं भारत की समृद्ध परम्परा से ही अपनी प्रेरणा लेती थीं,जिसके चलते इनमें अखिल भारतीय भावनाएं तथा राष्ट्रवाद उभरता था।
2. आधुनिक शिक्षा (पाश्चात्य शिक्षा) का प्रचलन
आधुनिक शिक्षा (पाश्चात्य शिक्षा) ने भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हांलाकि अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया था, किन्तु इसने शिक्षित भारतीयों को तार्किक, धर्म निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया।
भारतवासियों को मिल्टन, शैली, वायरन, बेन्थम, स्पेन्सर जैसे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने एक स्वर में ब्रिटिश निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठाई थी। वाल्टेयर, रूसो, मैजिनी आदि के विचारों ने भी भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया।
अंग्रेजी भाषा के प्रसार तथा लोकप्रियता से शिक्षित भारतीयों को एक सम्पर्क भाषा मिल गई, जिसके जरिए वे एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत करा सके तथा सम्मेलनों में भाग ले सके। प्राचीन काल में संस्कृत सम्पर्क भाषा का माध्यम थी किन्तु आधुनिक भारत में इसकी जगह अंग्रेजी ने ले ली। अंग्रेजी भाषा ने भारत की समस्त जातियों-धर्मों को एक मंच पर ला खड़ा किया।
3. प्रेस की भूमिका
भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में प्रेस की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। यद्यपि यूरोपीय लोगों के द्वारा ही सर्वप्रथम भारत में प्रेस स्थापित किए गए और समाचार पत्र एवं साहित्य प्रकाशित करना शुरू किया गया। किन्तु धीरे-धीरे भारतीय भाषा में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे।
हांलाकि समाचार पत्रों को अनेक दमनात्मक कानूनों का सामना करना पड़ा, फिर भी भारतीयों ने अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की। भारतीय समाचार पत्रों ने जनमत के उत्थान तथा राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई।
भारतीयों के राजनीतिक जीवन में जिन समाचार पत्रों ने अमिट छाप छोड़ी उनमें महत्वूर्ण थे — इंडियन मिरर, मम्बई समाचार, हिन्दू पैट्रियाट, अमृत बाजार पत्रिका, दि हिन्दू, दि बंगाली, बॉम्बे, क्रॉनिकल, मराठा, केसरी, इन्दु प्रकाश आदि। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय समाचार पत्रों ने भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण की भूमिका निभाई और जनता को शिक्षित करने का काम किया।
4. परिवहन तथा संचार साधनों का विकास
संचार साधनों के विकास जैसे- डाक, तार तथा रेल सेवाओं के विकास ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। रेलवे के कारण एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तथा ग्रामीण प्रदेश बड़े-बड़े नगरों से जुड़ गए। जबकि डाक व्यवस्था के चलते राष्ट्रीय साहित्य तथा सामाचार पत्र स्थान-स्थान पर भेजे जा सकते थे, जिससे भारतीयों के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला।
बिजली के तारों ने क्रांति पैदा कर दी। हांलाकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में इन साधनों का विकास अपनी प्रशासनिक सुविधा तथा व्यापारिक लाभ के लिए किया था किन्तु इन सुविधाओं के कारण भारतीयों में एक-दूसरे से सम्पर्क में वृद्धि हुई और वे अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध संगठित हुए।
5. अंग्रेजी राज का प्रभाव
अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण तथा अंग्रेजों की भूमि बन्दोबस्त नीति ने लाखों लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया।
ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शासकों ने साम्राज्यवाद के प्रसार तथा आर्थिक शोषण के लिए राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा बौद्धिक सभी क्षेत्रों में भारतीयों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति ने भी देशवासियों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया।
लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.सी.एस. परीक्षा की आयु में कमी, द्वितीय आंग्ल-युद्ध, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन आदि भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तात्कालिक कारण थे। रिपन द्वारा 1884 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य अंग्रेजों तथा भारतीयों को कानून की नजर में समाना बनाना था। इल्बर्ट बिल विवाद ने भारत में एक संगठित भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म दिया।
6. भारत की राजनीतिक एकता
साम्राज्यावादी इंग्लैण्ड ने सम्पूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर लिया, समस्त भारतीय प्रान्त तथा देशी रियासतें इनके अधीन थीं। लिहाजा पूरे देश में एक सी आधीनता, एक सी समस्याएं और एक ही कानून ने भारत को ब्रिटिश ढांचे में ढालना शुरू किया। देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत पर एक राजनीतिक एकता लाद दी थी। अंग्रेजों द्वारा देश में साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद भारतीयों की राजनीतिक एकता ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया।
7. भारत में शांति तथा प्रशासनिक एकता की स्थापना
अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी की अव्यवस्था के उपरान्त ब्रिटिश भारत में शांति तथा प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर ली थी। प्राय: अंग्रेज विद्वान इस तथ्य पर गर्व करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार दीर्घकालीन शांति स्थापित की गई थी।
भारतीय जनपद सेवा (आई.सी.एस.) के अत्यंत प्रशिक्षित एवं व्यावसायिक प्रशासक भारत के प्रत्येक हिस्से में प्रशासन चलाया करते थे। भारत के कोने-कोने में एक ही प्रकार का न्यायिक ढांचा, फौजदारी तथा दीवानी कानून का दृढ़ता से पालन होता था। इस व्यवस्था ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता भी प्रदान की।
8. मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय
भारत के मध्यमवर्गीय नागरिकों ने बड़ी तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली क्योंकि इससे ब्रिटिश नियुक्तियां प्राप्त करने में सुविधा हो जाती थी और दूसरों से सम्मान भी मिलता था। लिहाजा भारत का मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासनिक वर्ग के समीप होने के चलते अग्रणी बन गया।
यही मध्यम वर्ग आधुनिक भारत की नवीन आत्मा बन गया तथा इसने सम्पूर्ण भारत में अपनी शक्ति का संचार कर दिया। इसी वर्ग ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास एवं उसके सभी चरणों को नेतृत्व प्रदान किया।
9. जातिवाद
1857 की महाक्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी था कि शासकों तथा शासितों के मध्य एक जातीय कटुता आ चुकी थी। इंग्लैण्ड की प्रसिद्ध व्यंग्य पत्रिका ‘पंच’ (Punch) अपने चित्रों में भारतीयों को उपमानव जीव (आधा गोरिल्ला और आधा हब्शी) के रूप में प्रदर्शित करती थी, जिसे वरिष्ठ पाशविक शक्ति द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ एंग्लों- इंडियन नौकरशाहों के मन में यह धारणा बन चुकी थी कि भारतीयों के साथ केवल पाशविक बल की युक्ति ही कार्य करती है। इतना ही नहीं, अंग्रेज भारतीयों को एक निकृष्ट जाति का मानने लगे थे जो किसी विश्वास के पात्र नहीं थे। अंग्रजों की इस संकीर्ण मानसिकता के कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना जागृत हुई।
10. यूरोपीय आन्दोलनों का प्रभाव
उन दिनों स्पेन तथा पुर्तगाल के दक्षिणी अमरीका के साम्राज्यों के खण्डहरों पर अनेक राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो रहे थे। यूरोप में भी यूनान तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने तथा आयरलैण्ड के स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों के मनोभावों को अत्यधिक प्रभावित किया।
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने मेजिनी द्वारा शुरू किए गए ‘तरूण इटली’ आन्दोलन पर एवं गैरीबाल्डी और कार्बोनारी आन्दोलन पर व्याख्यान दिए तथा लेख लिखे। अत: यूरोपीय राष्ट्रवाद ने उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया।
11. आर्थिक शोषण
अंग्रेजी शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अत्यन्त विनाशकारी था। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं सदी के पूर्वाध में इंग्लैण्ड औद्यागिक क्रांति का अगुवा था, उसे अपने कच्चे मालों तथा तैयार माल के लिए एक मण्डी चाहिए थी। इसलिए साम्राज्यवादी इंग्लैण्ड की आवश्यकता यह थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का गठन औपनिवेशिक आदर्श पर किया जाए।
लिहाजा भारत की सभी आर्थिक नीतियां - कृषि, उद्योग, वित्त, शुल्क, विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय आदि, सभी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई।19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश भारत में कुल 24 अकाल पड़े, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ लोग कालकवलित हुए। बावजूद इसके अकाल के दिनों में भी अन्न भारत से निर्यात किया जाता रहा।
भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की बढ़ती दरिद्रता का मुख्य कारण अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीतियां ही बताया। उन्होंने दरिद्रता तथा विदेशी दासता को जोड़ दिया। इस मनोवृत्ति से विदेशी राज के प्रति घृणा पैदा हुई तथा स्वदेशी माल तथा स्वदेशी राज के प्रति प्रेम। इससे भारतीय राष्ट्रीयवाद को अत्यंत बढ़ावा मिला।
12. प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध का प्रभाव
पाश्चात्य विद्वानों सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, मैक्समूलर, रॉथ तथा सस्सन आदि द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध के परिणामस्वरूप जनता को भारत की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा का ज्ञान होने लगा।
विशेषकर लार्ड कनिंघम जैसे विद्वान पुरातत्वविदों ने भारत की महानता तथा गौरव का जो चित्र प्रस्तुत किया, वह रोम तथा यूनान की प्राचीन सभ्यताओं से किसी भी मामले में कम गौरवशाली नहीं था। कई यूरोपीय विद्वानों ने वेदों तथा उपनिषदों की साहित्यिक श्रेष्ठता का सुन्दर विश्लेषण तथा गुणगान किया।
इन्हीं यूरोपीय विद्वानों ने यह सिद्धान्त भी प्रस्तुत किया भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं, जिससे यूरोपीय जातियां उपजी हैं। इससे शिक्षित भारतीयों के आत्मसम्मान में एक मनोवैज्ञानिक बढ़ोतरी हुई। ऐसे में इन सभी तत्वों ने भारतीयों में देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया।
13. लार्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां
लार्ड लिटन की प्रतिक्रियात्मक नीतियों ने भारतवासियों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का काम किया। बतौर उदाहरण— आईसीएस में भर्ती होने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय शिक्षित युवक यह परीक्षा नहीं दे सकें।
साल 1877 में भीषण अकाल पड़ा था, ठीक उसी समय दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन कर लाखों रूपए खर्च किए गए। इस बारे में कलकत्ता के एक समाचार पत्र ने लिखा था - “नीरो वंशी बजा रहा था, जब रोम जल रहा था।” लार्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम तथा दो अन्य अधिनियम पारित किए जिससे जातीय कटुता ज्यादा बढ़ गई, परिणामस्वरूप भारत में अनेक राजनीतिक संस्थाएं बनीं ताकि सरकार विरोधी आन्दोलन चल सकें।
14. इल्बर्ट बिल विवाद
साल 1882 में ब्रिटिश हुकूमत ने यह कानून पारित किया कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अभियुक्तों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं रहा। इसी अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय के विधि सदस्य सर पी.सी इलबर्ट ने 2 फरवरी 1883 को एक विधेयक पेश किया जिसे ‘इलबर्ट बिल’ की संज्ञा दी जाती है।
इलबर्ट बिल विधेयक का उद्देश्य यह था कि “जातिभेद आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तत्काल समाप्त कर दी जाएं। इसके साथ ही भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं।” इस विधेयक के प्रस्तुत होते ही ब्रिटिश भारत में बवंडर खड़ा हो गया। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया।
यूरोपीय लोगों की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र और कटु थी कि वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा। इलबर्ट बिल विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी। यूरोपीय लोगों के विशेषाधिकार के प्रश्न पर भारतीयों की अनदेखी ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी प्रबल कर दिया।
इसे भी पढ़ें : भारत में वामपंथी आन्दोलन का उदय : साम्यवादी तथा कांग्रेस समाजवादी