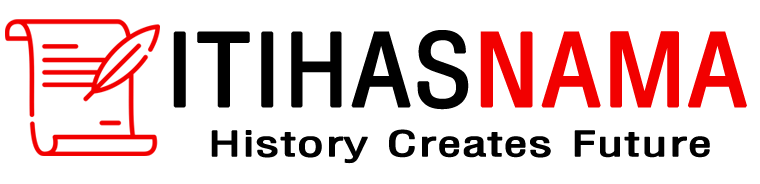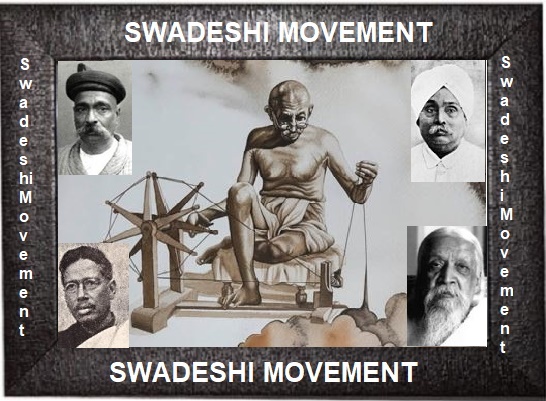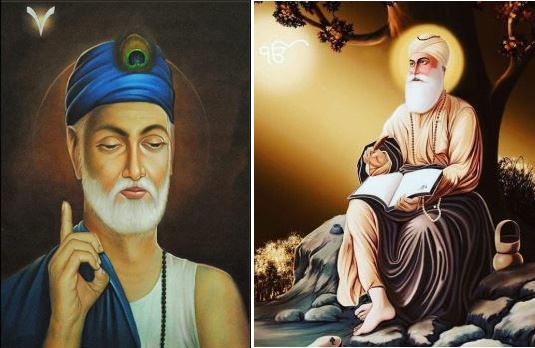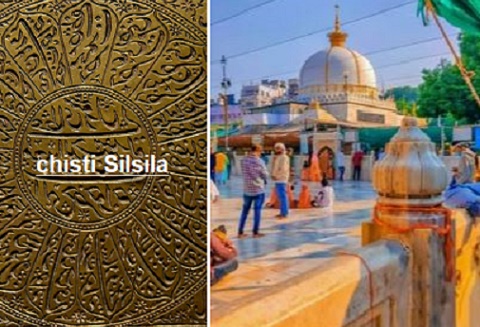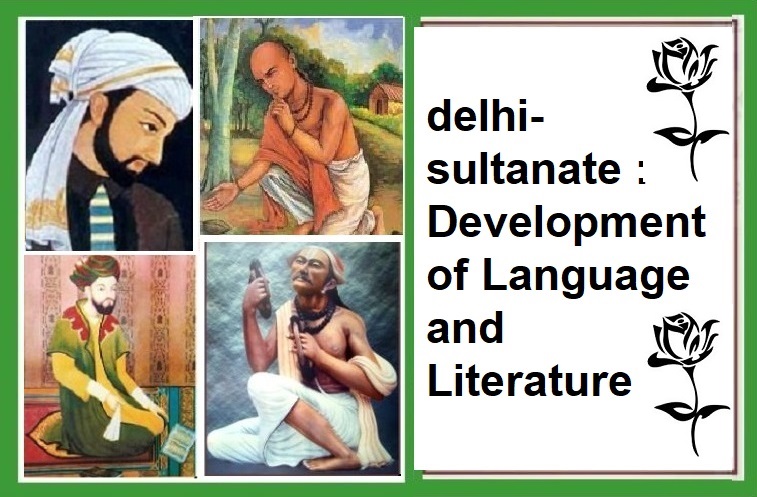
सल्तनत काल में फारसी एवं संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिन्दी, उर्दू तथा अन्य सभी प्रान्तीय भाषाओं में ग्रन्थ लिखे गए। सल्तनकाल में विभिन्न सुल्तानों के साथ-साथ अन्य प्रान्तीय शासकों ने भी विद्वानों को आश्रय प्रदान किए, परिणामस्वरूप धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई।
सल्तनत काल में गद्य, पद्य, नाटक आदि सभी प्रकार के पुस्तकों की रचना हुई, ऐसे में यह कहना लाजिमी होगा कि उन दिनों साहित्यिक प्रगति हुई थी। जहां तक फारसी साहित्य का प्रश्न है, इस भाषा पर धार्मिक कट्टरता का प्रभाव था जबकि संस्कृत साहित्य में मौलिकता का आभाव रहा, ज्यादातर पुस्तकें प्राचीन ग्रन्थों को आधार बनाकर लिखी गई थीं।
सल्तनत युग की मुख्य विशेषता विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के निर्माण का आधार तैयार करना था। हिन्दी, उर्दू, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी आदि प्रादेशिक भाषाओं को साहित्यिक भाषा का स्थान ग्रहण करने में समय अवश्य लगा परन्तु सल्तनतकाल में इसकी शुरूआत हो चुकी थी। प्रादेशिक भाषाओं को साहित्यिक भाषा का स्थान ग्रहण कराने में भक्ति आन्दोलन के संतों का योगदान सर्वाधिक रहा।
फारसी साहित्य
10वीं शताब्दी में भारत में तुर्कों के आगमन के साथ फारसी भाषा का प्रवेश हुआ। फारसी न केवल सल्तनतकाल बल्कि मुगलकाल में भी प्रशासन की भाषा थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने विभिन्न विद्वानों को राजाश्रय प्रदान कर फारसी साहित्य की प्रगति में सर्वाधिक योगदान दिया।
— सुल्तान इल्तुतमिश के समय नासिरी अबू-वक्र-बिन मुहम्मद रूहानी, ताजुद्दीन दबीर और नुरूद्दीन मुहम्मद मुख्य विद्वान थे। नुरूद्दीन मुहम्मद ने ‘लुबाब-उल-अल्बाब’ नामक ग्रंथ लिखा था।
— बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली फारसी साहित्य का मुख्य केन्द्र था।
— बलबन के पुत्र मुहम्मद ने अमीर खुसरव तथा मीर हसन देहलवी को राज्याश्रय प्रदान किया था।
— जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अमीर खुसरो की अध्यक्षता में फारसी के विकास हेतु राजकीय पुस्तकालय खोला।
— अमीर खुसरो सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि था जिसने अपनी कविताओं में ‘हिन्दी’ शब्दों का प्रयोग आरम्भ किया।
— अमीर खुसरो जैसे महान साहित्यकार को सल्तनकाल में 5 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त हुआ।
— अमीर खुसरो ने तकरीबन 92 ग्रन्थों की रचना की जिनमें मसनवी, खजाये-नुल-फुतूह, तुगलकनामा और तारीख-ए-अलाई, लैला-मजनूं, देवलरानी-खिज्रखां, हस्त-बहिस्त, नूह-ए-सिकन्दर आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं।
— सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के समय बदरूद्दीन मुहम्मद फारसी का श्रेष्ठ कवि था। मौलाना मुइनुद्दीन उमरानी तथा इसामी भी अन्य प्रख्यात विद्वान थे।
— सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के समय सूफी संत जियाउद्दीन नक्शवी ने फारसी ग्रन्थ ‘तूतीनामा’ की रचना की जो चिन्तामणि भट्ट की ‘शुक सप्तति’ का अनुवाद था। जियाउद्दीन नक्शवी ने कोकशास्त्र का भी फारसी अनुवाद किया।
— सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने स्वयं की आत्मकथा लिखी जिसका नाम ‘फुतूहात-ए-फिरोजशाही’ है।
— फिरोजशाह तुगलक ने जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए-सिराज-अफीफ को राजाश्रय प्रदान किया था।
— जियाउद्दीन बरनी ने ‘तारीख-ए-फिरोजशाही’ तथा ‘फतवा-ए-जहांदारी’ नामक प्रमुख ग्रन्थों की रचना की थी।
— लोदी सुल्तानों ने भी विद्वानों को खूब राजाश्रय प्रदान किए।
— सिकन्दर लोदी 'गुलरुखी' शीर्षक से फ़ारसी में कविताएँ लिखता था।
— रफीउद्दीन शिराजी, शेख अब्दुल्ला, और शेख जमालुद्दीन लोदी काल के मुख्य विद्वान थे।
— प्रान्तीय राज्यों के फारसी विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं- गुजरात में फजलुल्ला जैनुल आब्दीन, बिहार में इब्राहिम फारूखी, सिन्ध में सैयद मुईन-उल-हक, बहमनी शासकों में ताजुद्दीन फिरोजशाह और वहां के दरबारी मंत्रियों में महमूद गवां का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
संस्कृत साहित्य
विजयनगर, वारंगल और गुजरात के हिन्दू शासकों ने संस्कृत को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। सल्तनकाल में संस्कृत में काव्य, नाटक, दर्शन, टीकाएं आदि लिखी गईं परन्तु इस युग के ग्रन्थों में मौलिकता का अभाव रहा।
— प्रमुख हिन्दू राजाओं में हम्मीरदेव, प्रतापरूद्रदेव, वसन्तराज, वेमभूपाल, कात्यवेम, विरूपाक्ष, नरसिंह, कृष्णदेवराय, भूपाल आदि ने संस्कृत साहित्य का भरपूर पोषण किया।
— प्रतापरूद्रदेव के दरबारी विद्वान अगस्त्य ने ‘प्रतापरूद्रदेव यशोभूषन’, ‘कृष्ण-चरित्र’ आदि ग्रन्थों की रचना की।
— वीर वल्लाल तृतीय के संरक्षण में विद्याचक्रवर्तित तृतीय ने ‘रूक्मिणी कल्याण’ की रचना की।
— विजयनगर के शासक विरूपाक्ष के संरक्षण में माधव ने ‘नर्कासुर विजय’ की रचना की।
— वामनभट्ट वाण को महान विद्वान माना गया जिसने काव्य, नाटक, चरित, संदेश आदि विभिन्न प्रकार की रचनाएं की।
— विद्वान विद्यापति ने ‘दुर्गाभक्ति-तरंगिनी’ और अन्य ग्रन्थों की रचना की।
— जैन विद्वान जयचन्द्र ने हमीर-काव्य, विजयनगर के सम्राट विरूपाक्ष ने नारायण विलास, कृष्णदेवराय ने जाम्बवती -कल्याण तथा जयदेव ने गीतगोविन्द लिखा।
— जयसिंह सूरी कृत हम्मीर मद मर्दन, गंगाधर कृत गंगादास प्रताप विलास और रामानुज द्वारा ब्रह्मसूत्र पर लिखी टीकाएं भी उल्लेखनीय हैं।
— कवि सोमदेव ने ‘ललित विग्रहराज’ तथा राजा विग्रहराज चतुर्थ ने ‘हरिकेली’ नामक संस्कृत नाटक की रचना की।
— मनुस्मृति पर लिखी गई प्रख्यात टीका ‘मिताक्षरा’ की रचना करने वाले विद्वान विज्ञानेश्वर, दायभाग की रचना करने वाले जीमूतवाहन और ज्योतिष के महान विद्वान भाष्कराचार्य भी सल्तनतयुग के ही विद्वान थे।
— ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुल्तानों से संरक्षण प्राप्त नहीं होने के बावजूद तकरीबन सभी हिन्दू विद्वान अपने साहित्य को धनवान बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे।
हिन्दी साहित्य
खड़ीबोली और ब्रजभाषा हिन्दी के निर्माण का आधार बनी। चन्दबरदाई कृत पृथ्वीराजरासो हिन्दी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसकी शैली ‘पिंगल शैली’ है। सारंगधर का ‘हम्मीर काव्य’ तथा जगनिक कृत परमार रासो जिसे उत्तर प्रदेश में ‘आल्ह खंड’ कहा जाता है।
— 12वीं सदी में पं. दामोदर ने ‘उक्ति-व्यक्ति’ प्रकरण नामक ग्रन्थ अवधी भाषा में लिखा।
— 14वीं सदी में ‘वर्ण रत्नाकर’ नामक शब्दकोष की रचना की गई।
— शर्फुद्दीन यजदी रचित ‘जफरनामा’ में सर्वप्रथम हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया गया।
— 14वीं सदी में मुल्लादाउद ने अवधी भाषा में ‘चन्दायन’ नामक हिन्दी कविता की रचना की। जबकि मंझन ने ‘मधुमालती’ की रचना की।
— मलिक मुहम्मद जायसी ने ‘पदमावत’ हिन्दी में लिखा।
— मुस्लिम कवि कुतबन ने पौराणिक गाथाओं पर आधारित ग्रन्थ ‘मृगावती’ की रचना की।
— मैथिली साहित्य के विकास में विद्यापति ठाकुर का सर्वाधिक योगदान रहा।
उर्दू साहित्य
उर्दू मूलत: तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है- ‘शाही खेमा’ अथवा शिविर। सल्तनतकाल में उर्दू को ‘जबान-ए-हिन्दवी’ कहा जाता था। उर्दू का विकास फारसी, तुर्की, पंजाबी, अवधी व अन्य स्थानीय भाषाओं के संयोग से हुआ था। अमीर खुसरो उर्दू भाषा का पहला कवि माना जाता है।
दक्षिण में उर्दू के जिस रूप का विकास हुआ उसे दक्कनी कहा जाता है। उर्दू भाषा को ‘रेख्ता’ नाम से भी पुकारा जाता है। यद्यपि उर्दू भाषा का वास्तविक विकास 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में देखने को मिलता है।
सल्तनतकाल में क्षेत्रीय भाषाओं/साहित्य का विकास
भक्ति मार्ग के सन्तों तथा प्रचारकों ने विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के विकास में महती योगदान दिया। बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी, उड़िया, तमिल, कन्नड़, तेलुगू और मलयालम आदि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास इस युग में देखने को मिला।
बांग्ला साहित्य - सल्तनतकाल में बांग्ला साहित्य के विकास का श्रीगणेश विद्यापति और चंडीदास ने किया। इन्होंने श्रीकृष्ण को समर्पित अनेक ग्रन्थों की रचना की। सुल्तान नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का प्रथम बंगाली अनुवाद काशीरामदास से करवाया। बारबक शाह के काल में कृतिवास ने बंगाली में रामायण की अनुवाद किया। कृतिवास रामायण को ‘बंगाल का बाइबिल’ कहा जाता है। सुल्तान हुसैनशाह ने गीता का अनुवाद बंगाली भाषा में मालाधर बसु द्वारा करवाया। महाभारत के अश्वमेध पर्व के बांग्ला अनुवाद का श्रेय श्रीकर नंदी को जाता है। बांग्ला भाषा को लोकप्रिय बनाने वाले कवि का नाम चंडीदास है।
गुजराती साहित्य - मारवाड़ी, ब्रज और अन्य भाषाओं के मिश्रण से गुजराती भाषा की उत्पत्ति हुई। इस भाषा के विद्वानों में सर्वप्रथम जयानन्द सूरि, गुणरत्न सूरि आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिन्होंने ‘क्षेम प्रकाश’ व ‘भरत बाहुबली रास’ की रचना की। इस काल के अन्य ग्रन्थों में ‘हंसरास’, ‘बछरास’ और ‘शीलरास’ की रचना विजय सूरि द्वारा की गई। जबकि श्रीमुनि सुन्दर सूरि के द्वारा ‘शान्त रस’ की रचना की गई।
नरसिंह मेहता गुजरात में अपनी श्रीकृष्ण भक्ति के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हो गए। नरसिंह मेहता ने हरिमाला, सुदामा -चरित, चातुरी शोषण, सामदास नौविवाह आदि ग्रन्थों की रचना की। बाणभट्ट की कादम्बरी का गुजराती भाषा में अनुवाद भालन नामक कवि ने किया। 16वीं सदी तक गुजराती में गद्य का विकास होने लगा।
मराठी साहित्य - संत ज्ञानेश्वर ने गीता पर मराठी में टीकाएं लिखीं जिन्हें ‘ज्ञानेश्वरी’ कहा गया। मराठी साहित्य की श्रेष्ठ रचना है ज्ञानेश्वरी। सन्त एकनाथ ने ‘भागवत’ का मराठी अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त संत एकनाथ ने ‘रूक्मिणी स्वयंवर’ और ‘भावार्थ रामायण’ जैसे श्रेष्ठ मराठी ग्रन्थों की रचना की।
मराठी में दशोपन्त ने गीतार्णव, पदार्णव लिखा। मराठी साहित्य में संत तुकाराम के अभंगों को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। 12वीं सदी में मुकुन्दराज को मराठी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। मुकुन्दराज ने ‘विवेक सिन्ध’ की रचना की।
दक्षिण की अन्य भाषाएं -
हिन्दू साम्राज्य विजयनगर के शासकों के द्वारा तेलुगू भाषा के अनेक कवियों को संरक्षण प्रदान किया गया। विजयनगर का सम्राट कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान और विद्वानों का संरक्षक था।
कृष्णदेवराय ने राजनीति सिद्धान्त पर आधारित ‘अमुक्त माल्यद’ नामक महान ग्रन्थ की रचना की। उसके दरबार में तेलुगू के महान कवि अलसानी पेदन्ना ने मनुचरित की रचना की। उसी के दरबार के एक अन्य लेखक तिम्मण ने ‘पारिजात अपहरण’ नामक ग्रन्थ लिखा।
अन्य तेलुगू लेखकों में पोटाना जिसने भागवतपुराण का तेलुगू में अनुवाद किया। इसके बाद श्रीनाथ ने श्रीहर्ष रचित नेषधीय चरित काव्य का तेलुगू में अनुवाद किया। 14वीं सदी में तेलुगू का सबसे प्रसिद्ध कवि ऐरराप्रगदा था। उसने चम्पू शैली (गद्य-पद्य की मिश्रित शैली) में रामायण की रचना की।
कन्नड़ भाषा का प्रारम्भिक काल जैन सम्प्रदाय के लेखकों से प्रभावित रहा। रूद्रभट्ट ने चम्पू शैली में ‘जगन्नाथ विजय’ की रचना की। यह रचना संस्कृत ग्रन्थ विष्णु पुराण का रूपान्तरण है।
9वीं-10वीं सदी में सरलदास ने महाभारत का उड़िया में अनुवाद किया। वहीं बिल्लपुत्तुरार ने 13वीं सदी में महाभारत का तमिल अनुवाद प्रस्तुत किया जो भारतम कहलाया। अरूणागिरीनाथ ने मुरूगन देवता की प्रशंसा में भक्ति रचना तिरूप्पगल की रचना की।
सल्तनतकालीन भाषा एवं साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
. अरबी भाषा के ग्रन्थ चचनामा के लेखक का नाम है— अली अहमद।
. चचनामा में वर्णन किया गया है— सिन्ध विजय का।
. तारीख-ए-मासूमी का लेखक था— मीर मुहम्मद मासूम।
. तारीख-उल-हिन्द किसने लिखा है— अलबरूनी।
. जैन-उल-अखबार का लेखक था— अबू सईद।
. तारीख-उल-हिन्द का एक अन्य नाम है— किताब-उल-हिन्द।
. ताज-उल-मासिर नामक ग्रन्थ हसन निजामी ने तथा तबकात-ए-नासिरी के लेखक का नाम मिनहाज-उस-सिराज था।
. सुल्तान नासिरूद्दीन महमूद के समय दिल्ली का मुख्य काजी था— मिनहाज-उस-सिराज।
. तारीख-ए-फिरोजशाही, फतवा-ए-जहांदारी तथा मासीर नामक ग्रन्थ किसने लिखा था— जियाउद्दीन बरनी।
. फुतूह-उस-सलातीन का लेखक था— अबू मलिक इसामी।
. किताब-उल-रहला नामक ग्रन्थ लिखा था— इब्नबतूता ने।
. किताब-उल-रहला सम्बन्धित है— यात्रा वृत्तान्त से।
. तारीख-ए- फिरोजशाही लिखा था— शम्स-ए-सिराज अफीफ ने।
. तारीख-ए-मुबारकशाही नामक ग्रन्थ लिखा था — याहिया बिन अहमद सरहिन्दी ने।
. तारीख-ए-मुबारकशाही एकमात्र ऐतिहासिक ग्रन्थ है जिससे जानकारी मिलती है— सैय्यद वंश की।
. फारसी काव्य गुलरूखी लिखा था— सिकन्दर लोदी ने।
. लुवाब-उल-अल्बाब नामक ग्रन्थ लिखा था— नुरूद्दीन मुहम्मद ने।
. नुरूद्दीन मुहम्मद समकालीन था— इल्तुतमिश का।
. सल्तनतकाल में फारसी साहित्य का केन्द्र था— दिल्ली।
. सल्तनतकाल का प्रथम कवि जिसने अपनी काव्य रचनाओं में हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया था— अमीर खुसरो।
. मुहम्मद बिन तुगलक के समय का श्रेष्ठ कवि था— बदरूद्दीन मुहम्मद।
. नक्षत्रशास्त्र से जुड़े ग्रन्थ ‘दलयाले फिरोजशाही’ के लेखक का नाम— ऐजद्दीन खालिद किरमानी।
. मसनवी लिखने की परम्परा शुरू हुई— तुगलक काल से।
. अमीर खुसरो के गुरू का नाम— निजामुद्दीन औलिया।
. ईरानी तम्बूरा और भारतीय वीणा के संयोग से बना था— सितार।
. संस्कृत ग्रन्थ ‘शंकर विजय’ लिखा था— विद्यारण्य ने।
. संस्कृत ग्रन्थ ‘हम्मीर मद-मर्दन’ नामक ग्रन्थ लिखा था— जयसिंह सेरी ने।
. आल्हा खण्ड का लेखक था— जगनिक
. हिन्दी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का लेखक था— कवि चन्दबरदाई।
. हम्मीर रासो का लेखक था— सारंगधर।
. बीसलदेव रासो का लेखक— नरपति नाल्ह, खुमान रासो का लेखक था—दलपत विजय।